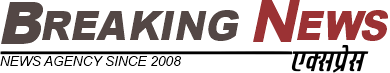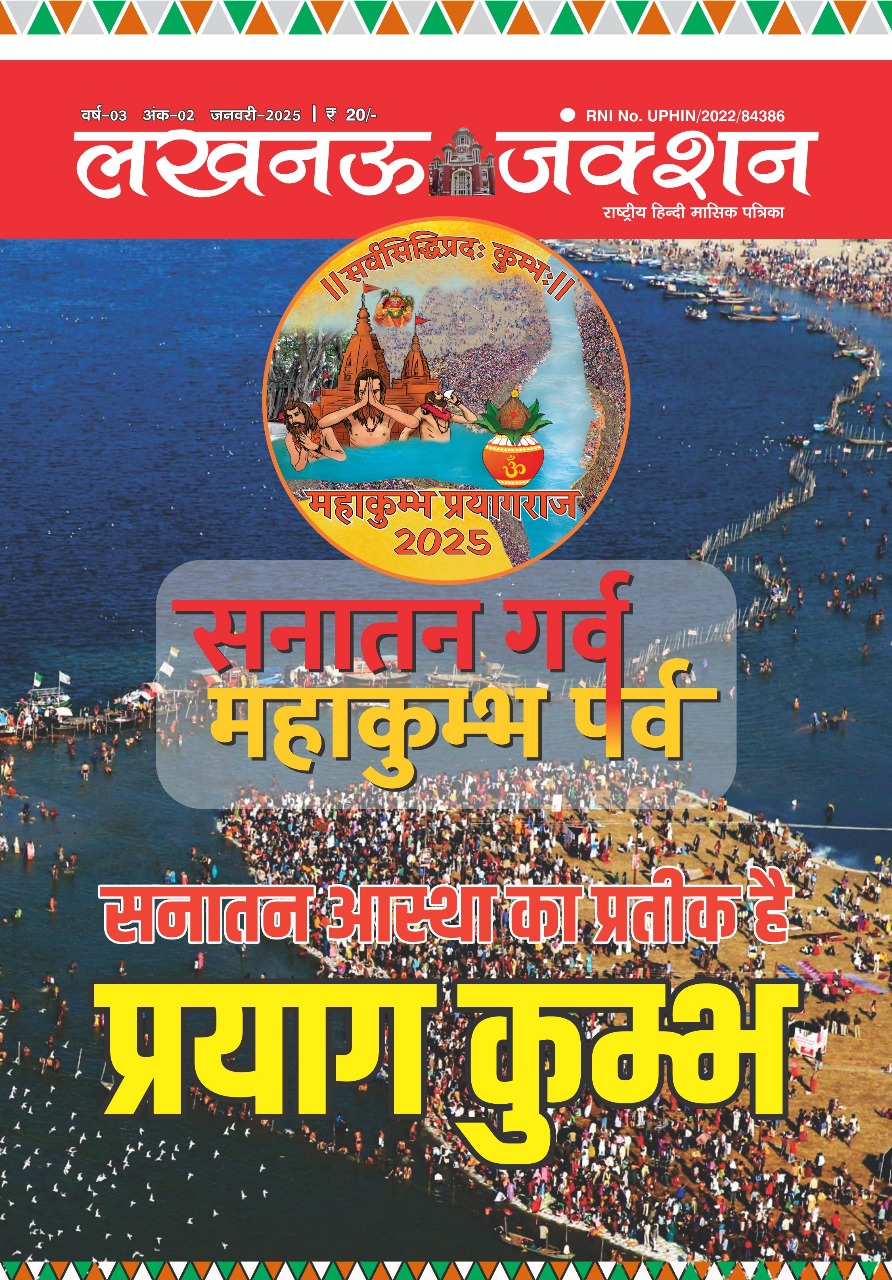पर्यावरण में ई-कचरे का गहराता संकट- विजय गर्ग
चुनौतियों और संभावनाओं को इक्कीसवीं सदी को प्लास्टिक और ई-कचरे की समस्या पिछली सदी से विरासत में मिली है। पिछली सदी में भले ही यह बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन इस सदी में इससे संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्लास्टिक के सामान और इलेक्ट्रानिक उपकरणों ने भले ही हमारे जीवन को सहूलियत भरा और आरामदायक बनाया है, लेकिन इसके नतीजे भी उतने ही भयावह नजर आने लगे हैं। आज जिस रफ्तार से प्लास्टिक और ई-कचरे का ढेर बढ़ रहा है, उससे साफ है कि ये अब पर्यावरण और मनुष्य दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। हालांकि, विश्व के विकसित देशों के मुकाबले भारत में प्लास्टिक की खपत काफी कम है, लेकिन आने वाले कुछ दशकों में इसमें तकरीबन छह छह गुना तेजी ‘आने का अनुमान है। माना रहा है कि वर्ष 2060 आते-आते हमारी प्लास्टिक खपत लगभग 16 शहरीकरण करोड़ मीट्रिक टन का आकड़ा छू लेगी। इसकी मुख्य वजह बढ़ता करण होगा। वर्ष 1990 में जहां हमारी प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत महज एक किलो थी, वहीं, वर्ष 2021 आते-आते हर व्यक्ति 15 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा था।
कचरा तकरीबन पांच करोड़ टन प्लास्टिक कचरा हर साल कूड़े के रूप में पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। पिछले साल भारत में नब्बे लाख टन से अधिक प्लास्टिक कचरा निकाला था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 में अलग-अलग राज्यों का प्लास्टिक कचरा चालीस लाख मीट्रिक टन था। पिछले वर्षों के मुकाबले इसमें 19 फीसद का इजाफा हुआ यह तो सिर्फ दर्ज आंकड़ा हो सकता है वास्तव में चौगुना हो। वर्ष 2024 में प्लास्टिक कचरा निकालने और फेंकने की रफ्तार में 21 फीसद की तेजी आई है। इसकी एक बड़ी वजह कचरे की निपटान व्यवस्था, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल में बुनियादी ढांचे की कमी है। प्लास्टिक कचरे का तकरीबन 40 फीसद हिस्सा कुप्रबंधन चलते कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाता है और यह शहरों के नालों से होकर नदी व नहरों से समंदर का रास्ता ले लेता है।
वर्ष 2022 में देशभर में 30 से 50 फीसद प्लास्टिक को दोबारा उपयोग में लाने का लक्ष्य भले ही रखा गया हो, लेकिन एक बार इस्तेमाल व्यवस्था के बावजूद समस्या प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने और जुर्माने का अभी तक जस की तस है। राज्य सरकारें भी इन खतरों को गंभीरता से लेती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब समस्या केवल प्लास्टिक के कचरे तक सीमित नहीं, बल्कि इसका नया साथी भी आ चुका है और वह है-
ई-कचरा यानी वे सारे उपकरण जो किसी न किसी रूप में बिजली संचालित होते हैं और खराब होने बदल दिए जाने की स्थिति में बाहर फेंक दिए जाते हैं। इनमें फोन, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, वाशिंग मशीन, बैटरी, प्रिंटर व मोबाइल इत्यादि शामिल है। इन उपकरणों को बनाने में जिन धातुओं का इस्तेमाल होता है, उनमें से ज्यादातर जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं।
भारत की बात करें तो यहां वर्ष 2012 में आठ लाख टन ई-कचरा निकाला था, ये सालाना दस फीसद की तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में सालाना पांच करोड़ टन ई-कचरा निकाला जाता है। भारत के कुल ई-कचरे का 70 फीसद हिस्सा केवल दस राज्यों से ही आ जाता है। केवल पैंसठ शहर देश के कुल कचरे में 60 फीसद से ज्यादा की हिस्सेदारी करते हैं। मुंबई इस सूची में आगे है और अन्य में दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पूणे, सूरत और नागपुर शामिल हैं। इसके अलावा भारत हर साल दूसरे देशों का ई-कचरा
भी खरीदता है। देश में औपचारिक तौर पर ई-कचरे का आयात प्रतिबंधित है, इसके बावजूद हमारे यहां सालाना पचास हजार टन ई-कचरा हर साल आयात होता है। मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात से सबसे ज्यादा कबाड़ भारत में आयात होता है। वर्ष 2022 में यह 39,800 मीट्रिक टन था। इसके अलावा यमन से हर साल 29,500 मीट्रिक टन कबाड़ का आयात होता है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 में यह केवल दस लाख मीट्रिक टन था, जो 2023-24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2019-2020 तक ई-कचरे में 72.54 फीसद की तेजी आई है। इसका एक कारण ये भी है कि इलेक्ट्रानिक सामान के आयात की बजाय अब देश में उत्पादन इकाइयों का तेजी से विस्तार हो रहा है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 में भारत का इलेक्ट्रानिक उत्पादन महज 5.54 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2023- 24 19.78 5 फीसद की तेजी के साथ 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चीन, अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा ई-कचरा उत्पादक देश है। हर साल लाखों की संख्या में मोबाइल फोन फेंके जाते हैं। भारत सालाना तीस लाख बीस हजार मीट्रिक टन ई-कचरा निकालता
है। । संयुक्त राष्ट्र की एक रपट के मुताबिक, वर्ष 2020 तक चीन में पुराने कंप्यूटरों से निकलने वाले ई-कचरे में 400 फीसद और भारत में 500 फीसद का का इजाफा हुआ। इसी तरह तकरीबन दो दशक पहले तक जहां केवल मोबाइल कचरा मात्र एक फीसद था, आज वह सारे ई-कचरे को पीछे छोड़ने की होड़ में है।
आज स्मार्टफोन आम से लेकर खास की जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है। नया माडल लेने की चाहत में लोग पुराने फोन तेजी से बदल रहे हैं। यह जरूरत नहीं, बल्कि शौक का मसला है। यह होड़ मोबाइल कचरे के ढेर को तेजी से बढ़ा रही है। स्मार्टफोन बनाने में कई तरह की धातुओं का इस्तेमाल होता है। धरती के नीचे इन धातुओं का खजाना धीरे-धीरे खाली रहा है, क्योंकि ये गैर-नवीकरणीय है। इनमें तांबा, सोना, निक्कल, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, चांदी, लिथियम व कोबाल्ट आदि शामिल है। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, डिजिटल कैमरे व एलईडी बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन ई-कचरे का बढ़ता ढेर और इलेक्ट्रानिक उत्पादों का सही ढंग से निस्तारण और दोबारा इस्तेमाल न पाना पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है।
हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके इन ई-उत्पादों में केवल प्लास्टिक, लोहा, जस्ता, सोना, चांदी वगैरह के अलावा लिथियम, सीसा, पारा आर्सेनिक, कैडमियम, कोबाल्ट और लैंड आदि जैसे जहरीले तत्त्व भी शामिल होते हैं। जो पर्यावरण और जलीय जीव-जंतुओं के लिए खतरनाक तो हैं ही, साथ ही इन्हें नष्ट करना भी आसान नहीं है। खराब होने के बाद इन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार करने से पहले इन धातुओं और तत्त्वों को अम्लीय सफाई से अलग करना जरूरी होता है। इस सफाई के बाद जो कचरा निकलता है, वह हवा, पानी, जमीन के जिस हिस्से में उतरता है, उसे जहरीला बना देता है। सवाल है कि सहूलियत से सजे इन ई-उपकरणों की चमकीली और रंगीन दुनिया में इनसे होने वाले खतरों से आंख मूंद कर क्या हम वाकई विकास की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे ?
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब