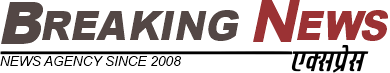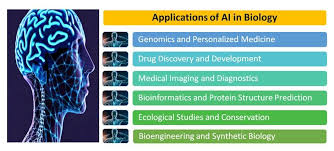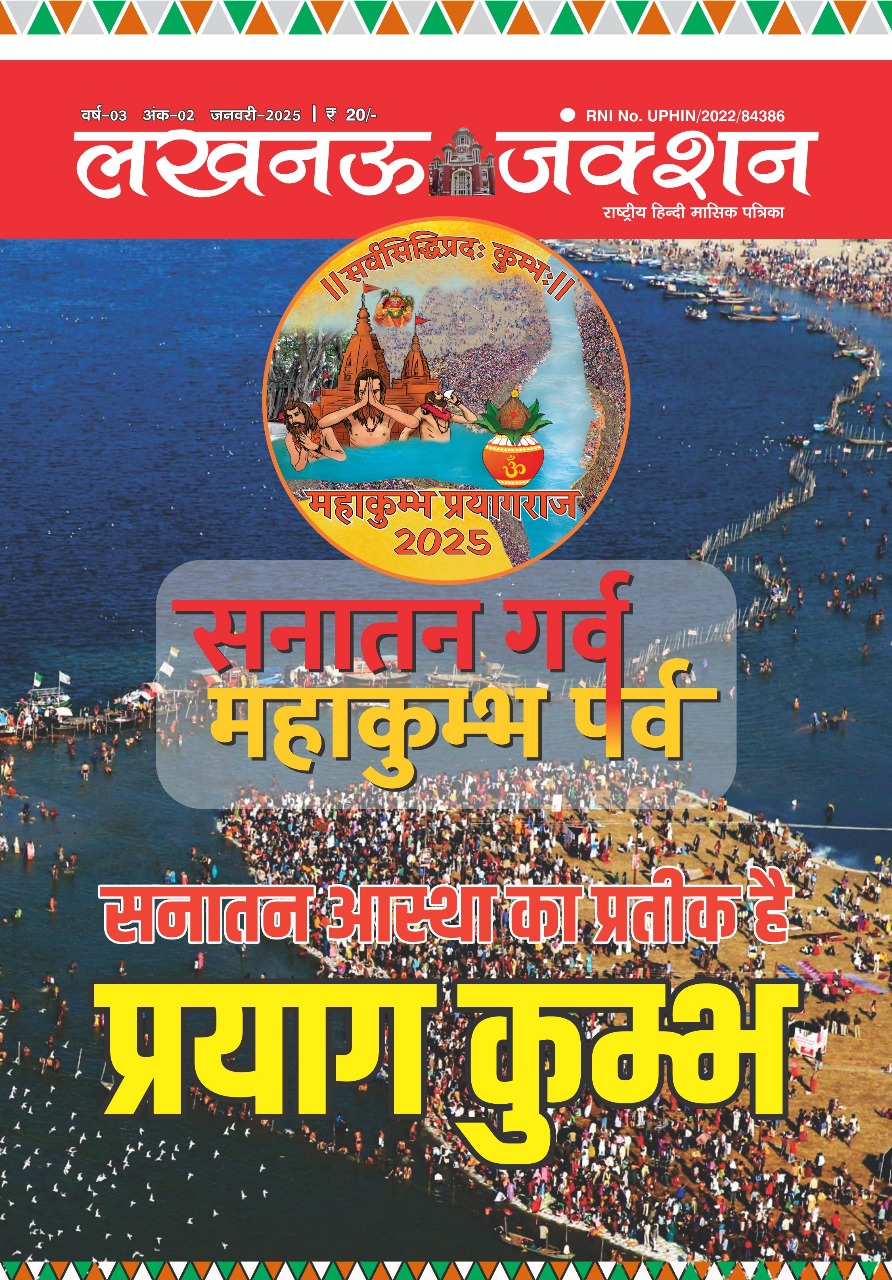कानून का राज या सत्ता का औजार? बृजेश चतुर्वेदी
भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव है कानून का राज। लेकिन संसद में हाल ही में सरकार द्वारा पेश किए गए आँकड़े इस नींव को हिला देने वाले हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले दस सालों में कुल 5892 मामले दर्ज किए। इनमें से केवल 1398 मामलों को ही अदालत में ट्रायल के लिए भेजा गया। यानी 77% मामलों में सबूत ही नहीं मिले और वे न्यायालय तक पहुँच ही नहीं पाए। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि कुल मामलों में से सिर्फ 8 मामलों में ही दोष सिद्ध हुआ। ईडी की कन्विक्शन दर मात्र 0.13% है। लगभग शून्य।
यह आँकड़ा केवल एक एजेंसी की नाकामी नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और न्याय-व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्नचिह्न है।
विधिक और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य
भारत का संविधान नागरिकों को समानता (अनुच्छेद 14), व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) और निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार देता है। प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत कार्य करता है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कसौटी पर कसा है और हाल में ही यह प्रश्न भी उठाया गया कि कहीं ईडी की गिरफ्तारी और तलाशी की शक्तियाँ नागरिक स्वतंत्रता का दमन तो नहीं बन रही हैं।
कानून का राज का अर्थ है कि सत्ता में बैठे लोग भी कानून के अधीन हों। लेकिन जब आँकड़े बताते हैं कि अधिकांश मामले राजनीतिक प्रतिशोध या दबाव का परिणाम हैं और अदालत में टिक नहीं पाते, तब यह रूल आफ ला नहीं बल्कि रूल बाई ला बन जाता है जहाँ कानून सत्ता का औजार बनकर नागरिकों को डराने-धमकाने का माध्यम भर रह जाता है।
लोकतंत्र पर प्रभाव
जब निर्दोष व्यक्ति वर्षों तक जाँच और मुकदमे में उलझते हैं, तो यह “न्याय में देरी” नहीं बल्कि “न्याय से वंचना” बन जाती है।
जाँच एजेंसियों की विश्वसनीयता तबाह हो जाती है और वास्तविक अपराधी भी बच निकलते हैं।
जनता का विश्वास कमज़ोर होता है और लोकतंत्र खोखला।
सुधार की ज़रूरत
1. एजेंसियों की स्वतंत्रता: ईडी और अन्य जाँच संस्थाओं को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त कर संसदीय समिति या लोकपाल के अधीन लाना चाहिए।
2. जवाबदेही तंत्र: जिन मामलों में बिना सबूत किसी को फँसाया गया, वहाँ अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो।
3. न्यायिक निगरानी: गंभीर मामलों में उच्च न्यायालय की निगरानी में जाँच अनिवार्य की जाए।
4. पारदर्शिता: चार्जशीट, केस की प्रगति और जाँच रिपोर्ट समय-समय पर सार्वजनिक हों।
5892 मामलों में केवल 8 दोष सिद्ध होना कोई संयोग नहीं, यह तंत्रगत विफलता है। यह स्थिति लोकतंत्र को “कानून के राज” से “सत्ता के राज” की ओर धकेल रही है। जनता को यह सवाल पूछना ही होगा—क्या जाँच एजेंसियाँ न्याय की प्रहरी हैं या राजनीतिक शस्त्र?
अगर कानून का राज सचमुच स्थापित करना है, तो अब समय आ गया है कि जाँच एजेंसियों को निष्पक्ष, जवाबदेह और संविधानसम्मत बनाया जाए। अन्यथा लोकतंत्र का यह स्तंभ भी सत्ता के भार तले चकनाचूर हो जाएगा।