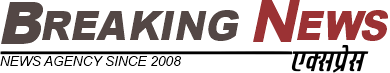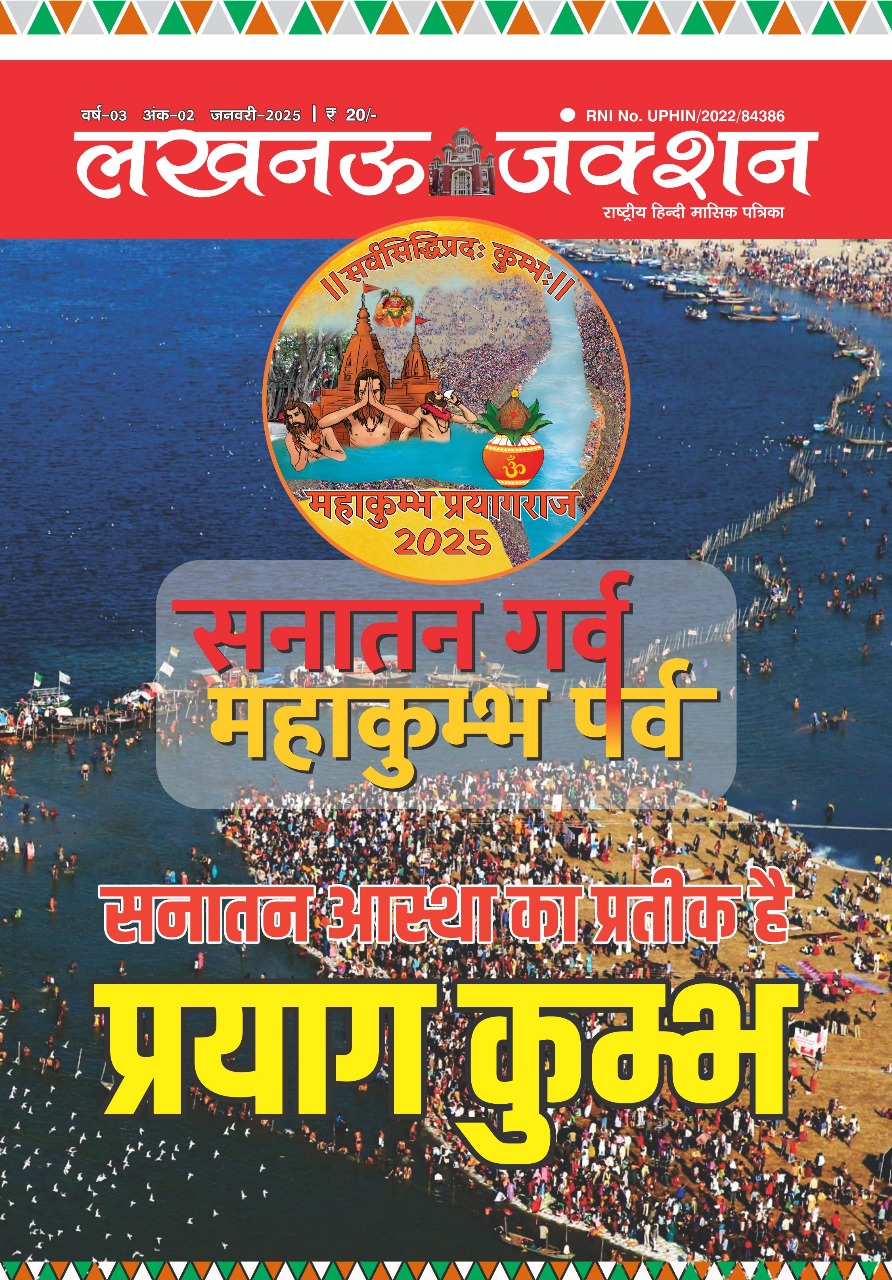खेल के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल
(महिला खिलाड़ी, दिव्यांगजन, आदिवासी और पारंपरिक खेलों को विशेष समर्थन मिलेगा)
विजय गर्ग
भारत में खेलों की परंपरा सदियों पुरानी है किसी गांव के धूल भरे अखाड़े से लेकर शहर के चमचमाते सिंथेटिक ट्रैक तक, हमारी साझी स्मृति में पसीने की गंध और माटी की सोंधी खुशबू बराबर रची-बसी है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इस पारंपरिक दृश्य के सामने एक नई रोशनी चमकी है, जैसे स्क्रीन, स्मार्ट रीडर और कलाइयों में लिपटी स्मार्ट-बैंड। बीते कुछ वर्षों में खेल का मैदान केवल खिलाड़ियों की मेहनत और अभ्यास का अखाड़ा नहीं रहा, बल्कि अब यह तकनीक की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। जहां पहले एक कोच की आंख और खिलाड़ी की संवेदनाएं प्रदर्शन को मापती थीं, वहीं आज कृत्रिम मेधा (एआइ) की आंखें, डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीकी उपकरण खेल के हर पल को बारीकी से पकड़ते हैं। ऐसे में उभरती खेल शक्ति के रूप में भारत के लिए यह बदलाव का अवसर भी है और चुनौती भी खिलाड़ी के शरीर का के हर सूक्ष्म कंपन अब डेटा है, जिसे ‘एल्गोरिदम’ पलक झपकते पढ़ लेते हैं।
हाल ही में जारी हुई ‘इंडिया एआइ मिशन और राष्ट्रीय खेल नीति-2025′ ने इस बदलाव को संस्थागत जामा पहना दिया है। खेल नीति दरअसल तीन बड़े वादों पर टिकी है। पहला, जनभागीदारी- मतलब हर बच्चे को कम से कम एक खेल से जोड़ना। दूसरा, उच्च प्रदर्शन- यानी वर्ष 2036 के ओलंपिक तक भारत पदकों की दहलीज पर खड़े रहने के बजाय ऊपर की सीढ़ियां चढ़े। तीसरा, खेल उद्योग का विकास- यानी खेल को करिअर, बाजार और नवाचार का पूर्णकालिक तंत्र बनाना। इन तीनों वादों को गति देने के लिए खेल नीति में कृत्रिम मेधा को ईंधन मान लिया गया है, जैसे किसी रथ को तीन घोड़े खींच रहे हों और कृत्रिम उनकी लगाम थामे सारथी हो। विद्यालयों में तंदरुस्ती संबंधी आंकड़े एकत्र करना, राज्यों में खेल विज्ञान केंद्र खोलना और निजी क्षेत्र को कर- रियायत देकर वाचार की राह चौड़ी करना, ये सब उसी विचार-श्रृंखला का हिस्सा हैं।
आज खिलाड़ी की तंदुरुस्ती का स्तर, हृदयगति, थकान, नींद और यहां तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी तकनीकी उपकरणों और साफ्टवेयर से मापी जाती है। फुटबाल, क्रिकेट और हाकी जैसे खेलों तो यह सामान्य बात हो गई है, लेकिन अब भारत जैसे देशों में कुश्ती, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे पारंपरिक खेलों में भी यह तकनीकी हस्तक्षेप दिखाई देने लगा है। ‘मशीन की आंख’ यानी कृत्रिम मेधा सिर्फ आंकड़े इकट्टा नहीं करती, बल्कि कोच और खेल संस्थानों को यह समझने में मदद करती है कि कौन-सा खिलाड़ी किस समय किस तरह का प्रदर्शन करेगा।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अब कबड्डी खिलाड़ियों को ‘स्मार्ट रीडर जैकेट पहनाई जाती है। इससे खिलाड़ी के कूदने, मुड़ने, सांस की गति, यहां तक कि पैंतरे बदलते वक्त उसकी आंखों की सूक्ष्म झपक भी दर्ज हो जाती है। लखनऊ की महिला हाकी अकादमी में ‘सेंसर स्टिक’ से पता चला कि ‘ड्रैग फ्लिक’ के समय ज्योति सिंह की दाहिनी कलाई जरूरत से अधिक घूमती है। एक हफ्ते में सुधार आया और उसने एशियन चैंपियंस ट्राफी में निर्णायक गोल दागा। पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारियों के दौरान फ्रांस और अमेरिका कृत्रिम मेधा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अमेरिका की जिम्नास्टिक टीम ने खिलाड़ियों की ‘बाडी मूवमेंट’ का थ्री डी विश्लेषण करने के लिए एक कृत्रिम मेधा उपकरण का इस्तेमाल कर व्यक्तिगत कमजोरियों की पहचान की और प्रशिक्षण को उसी मुताबिक बदला फ्रांस की साइक्लिंग टीम ने स्मार्ट हेलमेट का उपयोग कर खिलाड़ियों के दिल की धड़कन, आक्सीजन स्तर और थकान को मापा, जिससे उन्हें प्रतियोगिता के दौरान रणनीति बदलने में मदद मिली।
भारत की नई राष्ट्रीय खेल नीति में भी इस तकनीकी क्रांति को जगह दी गई है। सरकार ने कृत्रिम मेधा, डेटा विश्लेषण और खेल विज्ञान के
उपयोग को नीति के मूल में रखा है। इसका उद्देश्य सिर्फ ओलंपिक में पदक लाना नहीं है, बल्कि खेल को जन आंदोलन बनाना, युवाओं को सशक्त करना और देश को एक ‘फिट इंडिया’ में भी बदलना है। चयन प्रक्रिया में भी कृत्रिम मेधा ने बड़ा उलटफेर किया है। पूरे सत्र के प्रदर्शन का आंकड़ा खिलाड़ी की निरंतरता और तंदरुस्ती का सच सामने रख देता है। पारदर्शिता बढ़ी है और यह अच्छी बात है लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सुदूर क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ियों के पास अगर सेंसर-युक्त जूते नहीं हैं, तो उनकी दौड़ का ‘डेटा’ बनेगा कैसे? संभावना यह भी है कि गांव की कोई धाविका तकनीकी अभाव के के कारण चयन सूची से से बाहर रह रह सकती है। उधर, कृत्रिम मेधा ने | एक नया बाजार खोल दिया है- ‘स्पोर्ट्स टेक’ । केपीएमजी की एक रपट बताती है कि भारत का स्पोर्ट्स टेक बाजार 18 फीसद वार्षिक दर से बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक यह ढाई अरब डालर का हो जाएगा। नई नीति में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 50 फीसद पूंजीगत मदद की बात कही गई है। मगर बाजार के साथ जोखिम भी भी आते हैं। सबसे बड़ा खतरा निजी जानकारी की गोपनीयता का है। खिलाड़ी के हार्मोन, हृदय गति, नींद और सोशल मीडिया रुझान आदि के आंकड़े अगर सट्टेबाजों के हाथ लग जाएं, तो उनका करिअर तबाह हो सकता है। दूसरा, खतरा एल्गोरिदम के पूर्वाग्रह का है। अगर प्रशिक्षण आंकड़ा शहरों से आता है, तो मशीनी सीख इसी ढांचे को आदर्श मान लेगी। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी युवाओं द्वारा भाला फेंकने की ‘टुक्का थ्रो’ शैली को कृत्रिम मेधा आधारित कोचिंग प्रणाली ‘डिफार्म टेक्नीक’ मान सकती है, जबकि यह तकनीक उनकी कलाई की ताकत, वर्षों की स्थानीय अभ्यास विधि और क्षेत्रीय शारीरिक क्षमता का अनूठा उदाहरण है।
तीसरी चुनौती कोचिंग के ‘मानवीय कौशल’ से जुड़ी है। दशकों के अनुभव से प्रशिक्षक कभी-कभी ऐसा निर्णय लेते हैं, जिसे ‘डेटा’ नहीं पकड़ पाता। फुटबाल के मैच में कोच ने देखा कि उसका स्ट्राइकर भले ही थका लग रहा हो, मगर प्रतिद्वंद्वी उससे भी ज्यादा हांफ रहा है; कोच ने स्ट्राइकर को रुके रहने दिया और मैच पलट गया। अगर उस क्षण एल्गोरिदम का सुझाव सुनते, तो शायद बदलाव हो जाता और नतीजा अलग होता। इसीलिए जरूरी है कि अंतिम फैसला इंसानी विवेक का ही रहे। कृत्रिम मेधा सलाह दे, संचालक न बने। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खेल मानवीय त्रुटियों, भावनात्मक क्षणों और बेजोड़ हुनर का रंग खो देगा? जवाब है नहीं, अगर हम चेतन रहें। शतरंज के उदाहरण से अगर समझें तो कंप्यूटर के आने के बाद डर था कि खेल उबाऊ हो जाएगा, लेकिन मैग्नस और र विदित गुजराती जैसे खिलाड़ी उन्हीं इंजनों को चुनौती दे रहे हैं और नई रचनात्मक चालें ढूंढ़ रहे हैं।
हमें तीन सूत्र पकड़ने होंगे। पहला, ‘डेटा’ तक बराबर पहुंच- अगर संसाधन शहर के ही हिस्से हुए, तो सपने भी शहर तक सीमित रह जाएंगे। दूसरा, अंतिम निर्णय में इंसानी विवेक- एल्गोरिदम सलाह दे सकता है, मगर खेल की ‘कहानी’ इंसान ही लिखेगा। तीसरा, खिलाड़ी कल्याण- बीमा, मानसिक स्वास्थ्य, डेटा सुरक्षा सब एक ही ताने-बाने में बुने जाएं। खेल का उद्देश्य पदक ही नहीं, एक स्वस्थ और नैतिक समाज बनाना भी है। हालांकि, तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि कृत्रिम मेधा और डेटा एनालिटिक्स खिलाड़ियों के प्रदर्शन की रोज निगरानी होगी और सुधार के मौके समझ में आएंगे। महिला खिलाड़ी, दिव्यांगजन, आदिवासी और पारंपरिक खेलों को विशेष समर्थन मिलेगा, ताकि वे भी कामयाबी की यात्रा का हिस्सा बन सकें।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब