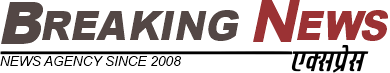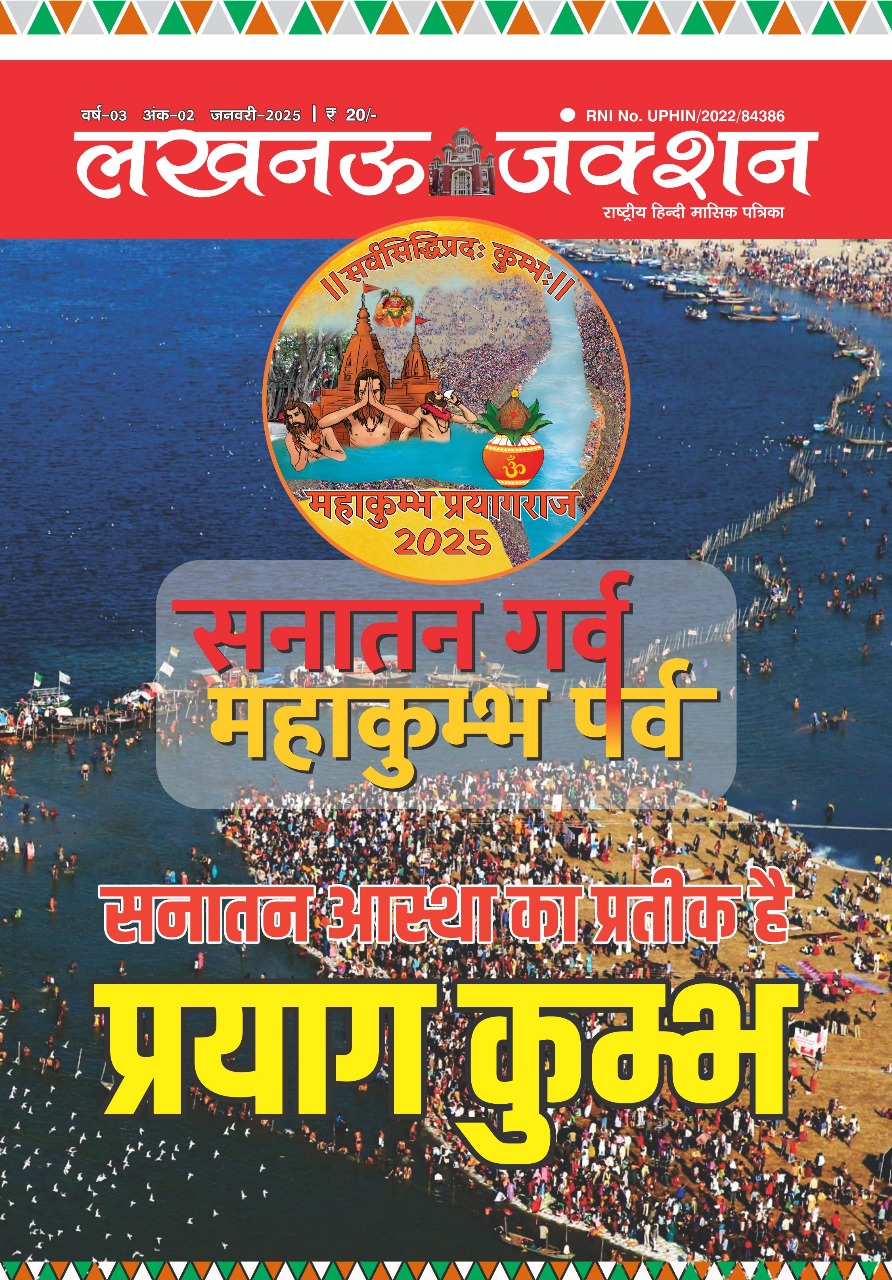जहां पहिया है -विजय गर्ग
साइकल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है? कुछ अजीब-सी बात है है न! लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले (तमिलनाडु) की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन को छोड़ने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई-न-कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी-कभी ये तरीके अजीबो-ग़रीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक ग़रीब जिले में से एक है पुडुकोट्टई। यहां की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकल को चुना है। उनमें से अधिकांशत नवसाक्षर थीं। अगर हम दस वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहां ग्रामीण महिलाओं के एक-चौथाई हिस्से ने साइकल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से सत्तर हज़ार से भी अधिक महिलाओं ने ‘प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता’ जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई ‘प्रशिक्षण शिविर’ चल रहे हैं।
ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा- ‘यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकल चलाना शुरू किया तो लोग फ़ब्तियां कसते थे। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।’ फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकल लेती हैं। एक नई साइकल ख़रीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि ‘साइकल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ेंगी।’ जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी- इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकल चलाना सिखाया है।
इस जिले में साइकल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मज़दूरी करनेवाली औरतें और गांवों में काम करनेवाली नसें बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशक़ीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचानेवाली औरतें भी पीछे नहीं हैं।
साइकल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, ‘मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकल पर चार किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी-कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहां तक कि साइकल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी-गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे- धीरे साइकल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। इसलिए • महिलाओं ने इसे अपना लिया।
साइकल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलाकुरुचि गांव में सभी साइकल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। ये नव- साइकल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है- ‘ओ बहिना, आ सीखें साइकल, घूमें समय के पहिए संग…’ जिन्हें साइकल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकल सीख चुकी महिलाएं अभी नई-नई साइकल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं।
1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफ़ान ला दिया। महिलाओं की साइकल चलाने की इस तैयारी ने यहां रहनेवालों को हक्का-बक्का कर दिया। साइकल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहां की कुछ महिलाएं अगल-बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। ख़राब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है। कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाक़ों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने- चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा मां साइकल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे दो या तीन बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है।
अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना ग़लत होगा। साइकल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है- ‘बेशक, यह मामला केवल आर्थिक नहीं है।’ फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा- ‘साइकल चलाने से मेरी कौन- सी कमाई होती है। मैं तो पैसे ही गंवाती हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकल ख़रीद सकूं। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और ख़ुशहाली का अनुभव कर सकूं।’ पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैने कभी साइकल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था।’
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब