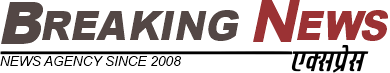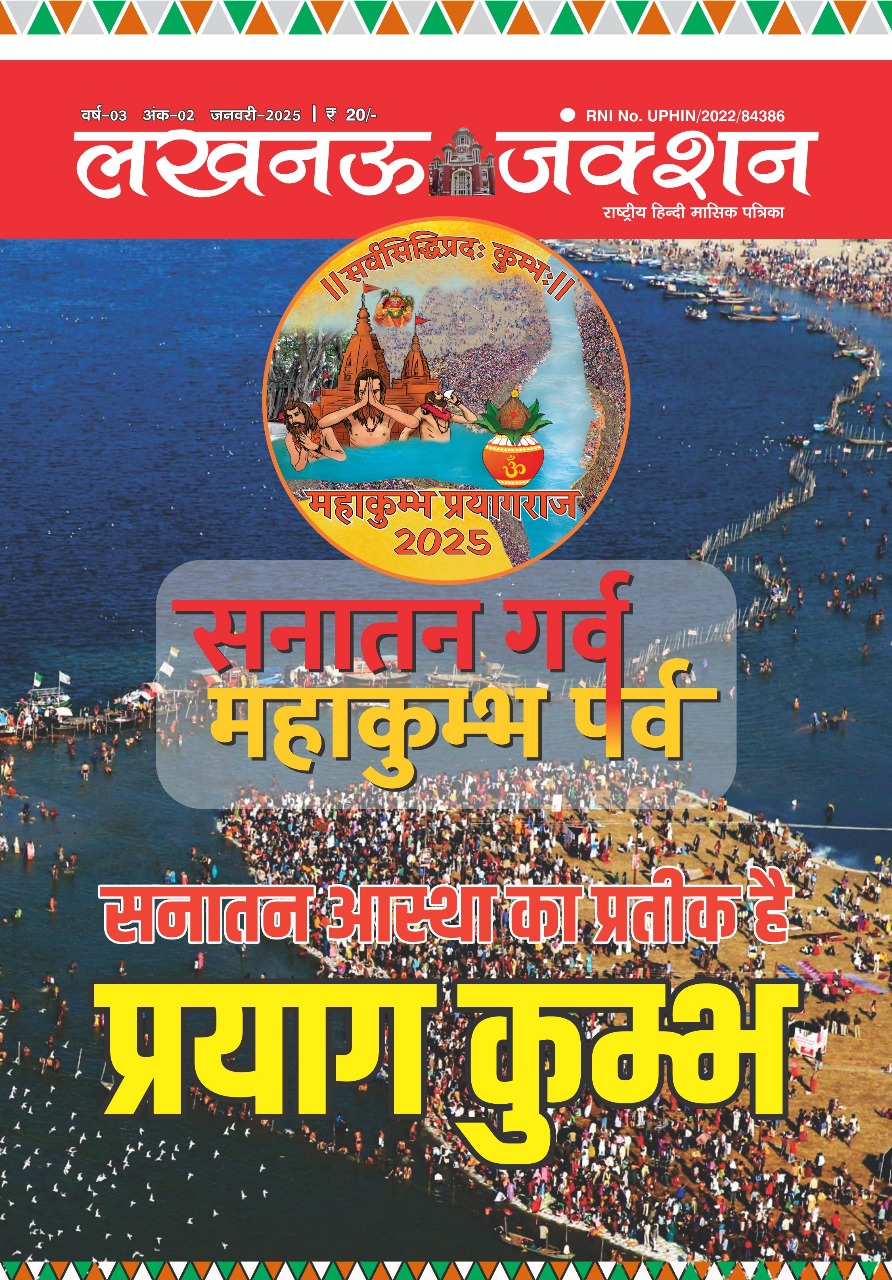फसलों में प्रयोग के खतरे -विजय गर्ग
शीर्ष न्यायालय में आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीएम फसलों के परीक्षण पर लगी रोक पर सुनवाई होनी है। पर्यावरण मंत्रालय की अनुमोदन समिति की संस्तुति ऐसी फसलों के लिए अनिवार्य होती है। उसी समिति ने इसे मंजूरी देने से इनकार किया है। संसद । अन्य दो समितियों की रपट में भी जीएम फसलों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभावों के आकलन के बिना मंजूरी न देने की बात कही गई है। देश में अभी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के रूप में केवल बीटी कपास की ही व्यावसायिक खेती हो रही रही है।
भारत की पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों की फसल धारा सरसों हाइब्रिड (डीएमएच-11 11) बीज के रूप में व्यावसायिक रूप से आवश्यक न्यूनतम मापदंड को पूरा करने में विफल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले रबी सीजन में छह अलग-अलग स्थानों पर किए गए क्षेत्रीय परीक्षणों के परिणामों के अनुसार डीएमएच-11 की उपज लगभग 26 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। कहा रहा है कि एक हजार बीजों पर यह लगभग 3.5 ग्राम है, जो कि बीज किस्म के रूप में अधिसूचना के पात्र होने के लिए 4.5 ग्राम के मानक से कम है। वैसे प्रति हजार पांच और 5.5 ग्राम से कम वजन वाले बीज सरसों की फसल की मशीनीकृत् कटाई को मुश्किल बनाते हैं। मशीनीकृत कटाई के दौरान कम वजन वाले सरसों के बीज उड़ जाते हैं। इसलिए उत्तरी क्षेत्र के किसानों द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता है।
अन्य व्यावसायिक संस्थानों के साथ-साथ नीति आयोग जीएम फसलों के लिए अड़ा हुआ है। कार्यबल की मसविदा रपट में दलहन एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जीएम बीजों के इस्तेमाल, बिजली पर सबसिडी को तर्कसंगत बनाने और किसानों को उपज के लिए घटे मूल्य पर भुगतान प्रणाली अपनाने की सिफारिश की जा चुकी है। जीएम फसलों के समर्थकों का एकमात्र तर्क यह है कि इसके प्रयोग से फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और देश की अनाज समस्या का समाधान हो जाएगा। निश्चित रूप से इससे कम अवधि के लिए फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है. लेकिन इसके दूरगामी परिणाम नुकसानदेह होते हैं। जीएम तकनीक के अंतर्गत बीजों के स्वजातीय जीन के आदान-प्रदान की प्रक्रिया नष्ट कर दूसरी प्रजाति जीन को समाहित किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया से तैयार बीज अप्राकृतिक और रासायनिक हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे अप्राकृतिक बता चुका है।
देश में अभी तक जीएम फसलों के रूप में बीटी कपास की व्यावसायिक खेती हो रही । वर्ष 2010 में बीटी बैंगन को भी मंजूरी दिलाने की कवायद शुरू हुई थी, पर नौ राज्य सरकारों, कई पर्यावरण विशेषज्ञों, कृषि विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और किसानों के व्यापक विरोध के कारण सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा। यहां तक कि स्वदेशी जागरण मंच और किसान संघ का तीव्र विरोध भी नीति निर्धारकों को झेलना पड़ा। मंच का कहना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। राजग सरकार के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार खुल कर इसके विरोध में आ गए हैं। उन्होंने पर्यावरण मंत्री को पत्र लिख कर कहा है कि जीएम बीज मामले में केंद्र सरकार को राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही इसको व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देनी चाहिए और राज्यों से बिना पूछे इसका किसी भी स्थान पर इसका परीक्षण न किया जाए।
यह एक गंभीर मामला है। सरसों बिहार का प्रमुख तिलहन है और बिहार देश के प्रमुख शहद उत्पादक राज्यों में शामिल है। नीतीश कुमार ने इस तकनीक को बाजार में उतारने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। पारंपरिक किस्मों की तुलना में जीएम किस्म को लेकर बढ़ा-चढ़ा कर दावे किए जा रहे हैं। मगर उसमें भी मतभेद हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि मौजूदा आइसीएआर की किस्म की उत्पादकता 2.1 टन प्रति हेक्टेयर है। जबकि रेपसीड और सरसों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 1.2 टन प्रति हेक्टेयर हैं।
विश्व के अन्य भागों में भी जीएम फसलों के परीक्षण अच्छे साबित नहीं हुए। अमेरिका में एक एक भू-भाग आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का की खेती की गई, जिसने 50 फीसद गैर-जीएम खेती को संक्रमित कर दिया। उत्पादन बढ़ाने की होड़ में चीन ने भी अपनी जमीन पर धान और मक्के की खेती की, मगर पांच-छह वर्षों में ही वहां के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 2014 के बाद वहां जीएम खेती लगभग बंद करनी पड़ी। जीएम फसलों के पैरोकार तीसरी दुनिया के मुल्कों को डरा रहे हैं कि वर्तमान में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, इसलिए जीएम फसलों के जरिए अतिरिक्त उत्पादन कर इसका मुकाबला संभव है। वर्तमान में भारत खाद्य उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो चला है, बल्कि गेहूं, धान, शक्कर, सब्जी एवं फलों आदि का बड़े पैमाने पर निर्यात भी कर रहा है।
सबसे खराब प्रयोग बीटी कपास के उत्पादन में हुआ, जिसे हम अभी भी झेल रहे हैं। वर्ष 2003 में देश में बीटी कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी मिली। बीटी कपास से देश के कपास उत्पादक किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर संसद की कृषि मामलों की समिति ने अपनी 37वीं रपट में काफी कुछ कहा । ‘कल्टीवेशन आफ जेनेटिक मोडिफाइड क्राप, संभावना एवं प्रभाव’ नामक रपट में बताया गया है कि बीटी कपास की व्यावसायिक खेती करने से कपास उत्पादक किसानों की माली हालत सुधरने के बजाय बिगड़ गई। इस कपास में कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना पड़ा।
महाराष्ट्र में इन दिनों अपनी कपास को कीड़े से बचाने की जुगत में किसानों द्वारा अनजाने में मौत को गले लगाने के कई मामले सामने आए हैं। अकेले यवतमाल जिले में ही चौबीस से अधिक किसानों की मौत के समाचार हैं। मौतों की वजह किसानों द्वारा खरीदा गया वह कीटनाशक बताया जा रहा है, जिसे उन्होंने फसल पर कीड़े मारने के लिए छिड़का था। बीटी कपास उगाने के लिए जिस कीटनाशक के उपयोग का प्रचार किया उस वक्त किसानों को यह बताया नहीं गया कि क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
वैज्ञानिक एमएस न स्वामीनाथन आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के प्रयोग से पहले भूमि परीक्षण अनिवार्य करने की सिफारिश कर चुके हैं। आश्चर्यजनक है कि किसानों को गोलबंद करने वाला महाराष्ट्र शेतकारी संगठन जीएम फसलों का गुणगान करने में जुटा है। जबकि दिलचस्प है कि किसान आत्महत्या की सर्वाधिक खबरें विदर्भ और मराठवाड़ा से ही आ रही हैं। पर्यावरण समर्थकों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने जीएम फसलों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सशर्त मंजूरी देने के केंद्र के फैसले की वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया था। हालांकि इसने केंद्र को इन फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का भी निर्देश दिया।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब