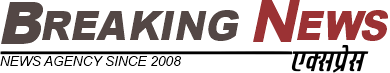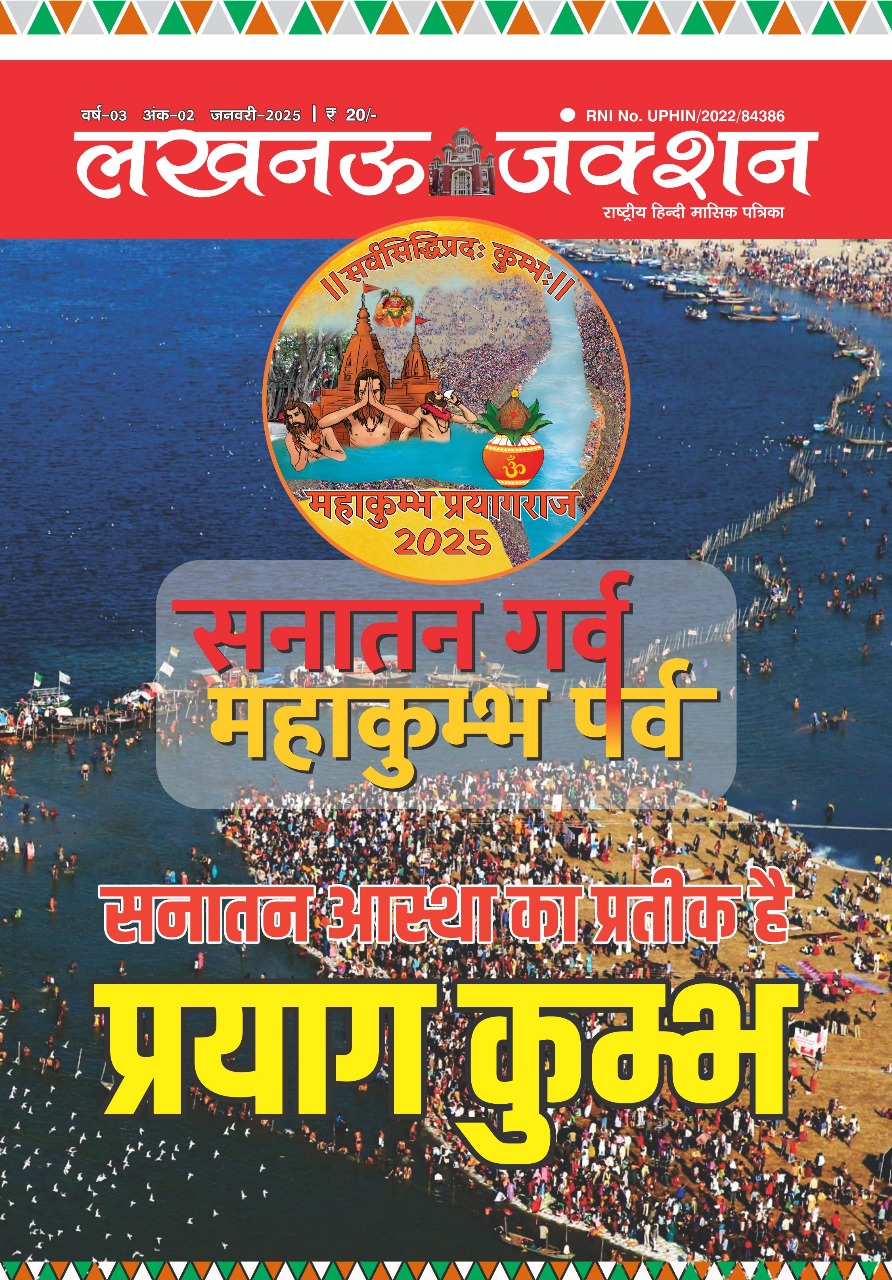हवा में घुलते धूलकणों से बाधित सांसें- विजय गर्ग
दिल्ली की दमघोंटू हवा अब किसी एक मौसम की समस्या नहीं रही। सड़कों पर उठती धूल, निर्माण स्थलों से उड़ती रेत और प्रदूषण के बादल अब न सीमाओं में कैद हैं, न मौसम की चेतावनी में सिमटे हर वर्ष लगभग 200 करोड़ टन धूल वातावरण में घुल रही है और इसका असर दुनिया भर में 380 करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ रहा है। ये आंकड़े चेतावनी नहीं, एक ‘अनदेखे युद्ध’ की घोषणा है, जहां दुश्मन हवा में घुला है और उसके हथियार हमारे फेफड़ों को निशाना बना रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) की रपट इस वैश्विक चुनौती की गंभीरता को और स्पष्ट करती है। इन धूलकणों का आकार चाहे जितना भी सूक्ष्म हो, इनका प्रभाव शरीर में गहराई तक जाता है। ये श्वसन तंत्र को स्थायी क्षति पहुंचाते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रपटें अब साफ संकेत दे रही हैं कि धूल भरे तूफान अब प्राकृतिक घटनाएं नहीं, वैश्विक आपदा के रूप में सामने हैं, जिनका प्रभाव अब हर महाद्वीप, हर देश और हर नागरिक झेल रहा है। ‘एअरबोर्न डस्ट बुलेटिन’ के अनुसार, हर वर्ष लगभग डेढ़ सौ देशों के तैंतीस करोड़ से अधिक लोग धूल भरी आंधियों के प्रभाव में आते हैं। यह संकट न केवल मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है, बल्कि कृषि, जलवायु और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। हर वर्ष कई लाख लोगों की मृत्यु धूल से उत्पन्न स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण होती है। आंकड़े भयावह हैं। दिल्ली जैसे शहरों में ‘पार्टिकुलेट मैटर’ (पीएम-10) और पीएम 2.5 के स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक हैं। सांस लेना अब मुश्किल होता जा रहा है।
सवाल है कि क्या साफ हवा अब विशेषाधिकार बन रही है? यह सवाल अब केवल नीतिगत चर्चाओं का विषय नहीं रहा। यह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। जब बच्चों को स्कूल जाते समय मास्क पहनना पड़ता है,
जब बुजुर्ग घर के भीतर भी हांफते हैं, तब यह मुद्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा बन जाता है। डब्लूएमओ की रपट बताती है कि रेत और धूल की आंधियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2018 से 2022 के बीच करोड़ों लोग इन खतरनाक धूलकणों के संपर्क में आए। ‘यूएस जियोलाजिकल सर्वे’ और लैंसेट’ की रपट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017 में अमेरिका में धूल के कारण भारी नुकसान हुआ, यह वर्ष 1995 की तुलना में चार गुना अधिक था। वर्ष 2024 में स्पेन के कैनरी द्वीप, मंगोलिया और पूर्वी एशिया में आए बड़े तूफानों ने में पीएम 10 का स्तर 1000 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से भी ऊपर पहुंचा दिया।
दिल्ली में भी ऐसे आंकड़े कोई असामान्य नहीं। फर्क केवल इतना है कि वहां दस्तावेज बनते यहां चुप्पी साध ली जाती है। भारत में वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। यह नुकसान केवल आंकड़ों में नहीं झलकता, यह उन खेतों में दिखता है, जहां फसलें मुरझा रही हैं, उन नदियों में दिखता है जहां धूलकण गिर कर जल को विषैला बना रहे हैं और उन बच्चों की आंखों में दिखता है जो सांस लेने के लिए दवाओं पर निर्भर हो चुके हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार धूल भरी आंधियों वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन में 20 से 25 फीसद तक की गिरावट आती है।
भारत में अधिकृत आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लगभग 40 लाख से अधिक निर्माण स्थल सक्रिय रहते हैं, जो किसी न किसी रूप में धूल प्रदूषण बढ़ाते हैं। यह केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं, एक सामाजिक त्रासदी भी बन चुका है। सरकारों द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) जैसी योजनाएं लाई गई हैं, जिनका उद्देश्य 2024 तक प्रमुख शहरों में प्रदूषण को 20 से 30 फीसद तक कम करना था। फिर भी अधिकांश स्वतंत्र रपटें यही दिखाती हैं कि इन योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन बेहद धीमा नीति और वास्तविकता के बीच जो खाई है, उसमें रोज नागरिक की सांसें डूब रही हैं। पारदर्शिता और स्थानीय भागीदारी की कमी इन योजनाओं को कागजी बना रही है।
और वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं होता। यह मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, जिससे खेती संकट में आती है। हवा में घुलने वाला यह जहर जल स्रोतों को भी विषैला बनाता है। गांवों और कस्बों में जहां प्रदूषण की निगरानी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं, वहां यह और घातक हो जाता है। कुल मिला कर यह संकट अब त्रि- आयामी हो चुका है। स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों पर इसकी गहरी चोट है। जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, अनियमि वर्षा और मानव जनित गतिविधियां धूल के तूफानों की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा रही हैं। यह मान लेना कि यह केवल प्राकृतिक आपदा एक प्रकार से बड़ी भूल होगी। इन तूफानों की उत्पत्ति में मानव की भूमिका स्पष्ट है जब जंगल काटे जाते हैं, जब निर्माण गतिविधियां नियंत्रण से बाहर होती हैं, जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में हरित पट्टी योजना ठप पड़ती है, तब धूल अपना साम्राज्य फैलाती है।
अब समय आ गया है कि स्वच्छ हवा को अधिकार मानते हुए उसके संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य किए जाएं। नीति निर्माण से लेकर जीवनशैली तक, हर स्तर पर बदलाव जरूरी है। हमें मास्क पहन कर जीने की आदत नहीं डालनी, हमें मास्क की आवश्यकता ही समाप्त करनी है। स्कूलों और कालेजों में पर्यावरणीय शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखना, उसे व्यवहार में उतारना होगा। नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। चाहे वह गाड़ी का कम इस्तेमाल हो, कचरे का सही निस्तारण हो या वृक्षारोपण हो। सरकारों
जवाबदेही की मांग जरूरी है। जब तक नीति-निर्माता यह नहीं समझ स्वच्छ हवा मौलिक अधिकार है, तब तक बदलाव क कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
स्वच्छ हवा की यह लड़ाई केवल पर्यावरण की नहीं, नैतिकता की भी है। यह उस सभ्यता पर सवाल है जो विकास के नाम पर अपने ही जीवित है और जहरीले कणों के बीच अगर हमें तंतुओं को काट रही है। धूल, धुएं जीने की आदत डालनी पड़ रही है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हमने अपने भविष्य की कीमत आज की सुविधा से चुका है। यह संकट कोई अचानक आई आपदा नहीं, जो हमारी चुप्पियों और उदासीनता की देन है। हवा कोई अदृश्य सुविधा नहीं, यह सजीव संसाधन है, जिसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सवाल यह नहीं कि हम कब कार्रवाई करेंगे, सवाल यह है कि क्या तब भी कुछ बचा होगा, जब हम कार्रवाई के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अगर हम अब भी नहीं चेते, तो वह दिन दूर नहीं जब धूल का यह साम्राज्य हमारी चेतना को इस हद तक जकड़ लेगा कि हम सवाल पूछना भी भूल जाएंगे। यह प्रश्न अब टालने योग्य नहीं तो क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं?
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब
++-++++++++++++++++++