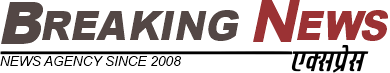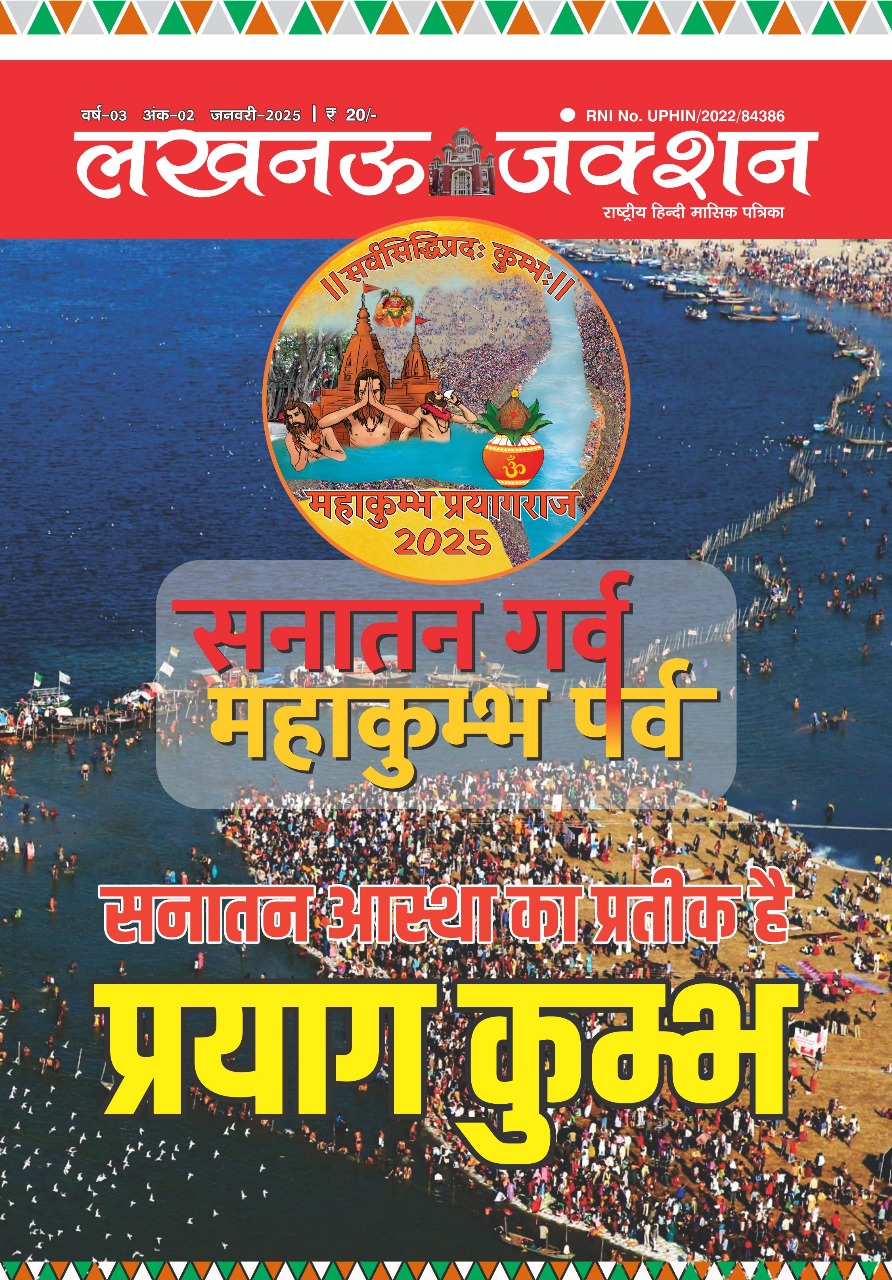ग्रामीण विकास को गति देती पंचायतें- विजय गर्ग
भारत में पंचायत को सुशासन की दृष्टि से देखें, तो लोक सशक्तीकरण इसकी पूर्णता है और लोक विकेंद्रीकरण की नजर से देखें, तो यह एक ग्रामीण स्वशासन की परिपाटी की पूर्ति है जो ग्रामीण विकास के लिए कहीं अधिक जरूरी है। इतना ही नहीं यह गांधी के ग्राम- स्वराज के सपने को भी बल देता है। सुशासन शांति और खुशहाली का परिचायक है। जबकि पंचायत एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण स्वराज को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 6.65 लाख गांव हैं, जिनमें 2.68 लाख ग्राम पंचायतें और ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, जो देश के ग्रामीण परिदृश्य का आधार हैं। पंचायतें ग्रामीण विकास को गति दे ही रही हैं, आम आदमी की भी ताकत बन रही हैं।
केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास को रफ्तार देने और केंद्रित कार्यक्रमों तथा निवेशों के जरिए समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहल की गई। मसलन वर्ष 2028 तक के लिए जीवन मिशन, ब्राडबैंड सुविधा, जिसका लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इंटरनेट पहुंच उपलब्ध हो तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय डाक उद्यमियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने वाले एक प्रमुख सार्वजनिक ‘लाजिस्टिक्स’ संगठन के रूप में विकसित करना भी लक्ष्य है। ग्रामीण समृद्धि एवं अनुकूलन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, हाशिए पर पड़े समुदायों और भूमिहीन परिवारों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।
पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी नींव है। पंचायत जैसी संस्था की बनावट कई प्रयोगों और अनुप्रयोगों का भी नतीजा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विफल होना और इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति का गठन फिर वर्ष 1957 में उसी की रपट पर इसका मूर्त रूप लेना देखा जा सकता है। गौरतलब है कि जिस पंचायत को राजनीति से परे और नीति उन्मुख सजग प्रहरी की भूमिका में समस्या दूर करने का एक माध्यम माना जाता है, आज वही कई समस्याओं से जकड़ी हुई है। जिस पंचायत ने सबसे नीचे के लोकतंत्र को कंधा दिया हुआ है, वही कई जंजालों से मुक्त नहीं है, चाहे वित्तीय संकट हो या उचित नियोजन की कमी या फिर अशिक्षा, रूढ़िवादिता तथा पुरुष वर्चस्व के के साथ जाति और ऊंच-नीच के पूर्वाग्रह ही क्यों न हों। यह समस्या पिछले तीन दशकों में घटी तो है और इसी पंचायत यह सिद्ध भी किया है कि उसका कोई विकल्प नहीं है।
पंचायत की । व्याख्या में क्षेत्र विशेष में शासन करने का विशिष्ट अधिकार निहित है। इसी अधिकार से उन दायित्वों की पूर्ति होती है जो ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत स्वशासन का बहाव भरता है और ग्रामीण बदलाव की गाढ़ी रेखा खींचता है। वर्ष 1997 का नागरिक घोषणापत्र सुशासन का ही शिखर था और 2005 में सूचना का अधिकार इसी का अगला अध्याय इतना ही नहीं वर्ष 2006 की ई-गवर्नेस योजना भी सुशासन की रूपरेखा को ही विस्तृत नहीं करती, बल्कि इनसे पंचायत को भी ताकत मिलती है। वर्ष 1992 में सुशासन की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन में सामने आई थी। वर्ष 1991 में उदारीकरण के बाद इसकी पहल भारत में भी देखी गई। सुशासन के इसी वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया जा रहा था। संविधान के 73वें संशोधन में जब इसे संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तब वर्ष 1959 से राजस्थान के नागौर से यात्रा कर रही यह पंचायत रूपी संस्था नए आभामंडल से युक्त हो गई। वर्ष 1992 में हुए इस संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया।
स्वशासन के संस्थान के रूप में इसकी व्याख्या दो तरीके से की जा सकती है। पहला संविधान में इसे सुशासन के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका सीधा मतलब स्वायत्तता और क्षेत्र विशेष में शासन करने का पूर्ण अधिकार है। दूसरा यह प्रशासनिक संघीयकरण को मजबूत करता है। गौरतलब है कि संविधान के इसी संशोधन में गांधी के ग्राम स्वराज को पूरा किया, मगर क्या यह बात भी पूरी शिद्दत से कही जा सकती है कि स्वतंत्र भारत की अति महत्त्वाकांक्षी संस्था स्थानीय स्वशासन से परिपूर्ण है। पंचायतों में एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण इसी संशोधन के साथ सुनिश्चित कर दिया गया था जो मौजूदा समय में पचास फीसद तक है। देखा जाए तो तीन दशक से अधिक पुरानी संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति रूढ़िवादी सोच में अच्छा खासा बदलाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वे भय, संकोच और घबराहट को दूर करने में कामयाब भी रही हैं।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम है कि पंचायतों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। महिलाओं की भागीदारी भी सामने आ रही है। मगर राजनीतिक माहौल में अपराधीकरण, बाहुबल, जातिवाद और ऊंच-नीच आदि दुर्गुणों से पंचायतें मुक्त नहीं है। समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन भी शासन की एक कड़ी है। इसका लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करना जहां शोषण और सुशासन का प्रभाव हो, जिससे पंचायत में पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके। वर्ष 2011 1 की जनगणना के अनुसार देश में चौथा व्यक्ति अभी भी अशिक्षित है। पंचायत और सुशासन पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कई महिला प्रतिनिधि ऐसी हैं जिनको पंचायत के नियम पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है। डिजिटल इंडिया का संदर्भ भी 2015 से देखा जा सकता है। आनलाइन क्रियाकलाप और डिजिटलीकरण ने पंचायत से जुड़े ऐसे प्रतिनिधियों के लिए कमोबेश चुनौती पैदा है। हालांकि देश की ढाई लाख से अधिक पंचायतों में काफी हद तक डिजिटल संपर्क बाकी है। साथ ही बिजली आदि की आपूर्ति का कमजोर होना भी इसमें एक बाधा है।
• डिजिटल क्रांति ने सुशासन पर गहरी छाप छोड़ी है। डिजिटल लेन-देन में तेजी आई है, कागजों के आदान-प्रदान में बढ़ोतरी हुई है, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो रहा है। फसल बीमा कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं में दावों के निपटारे के लिए ‘रिमोट सेंसिंग’, एआइ और ‘माडलिंग टूल्स’ का प्रयोग होने लगा है। वहीं ग्राम पंचायतों में खुले स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे ग्राम स्तरीय उद्यमी बनें सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं का पूर्ण रूपांतरण ही ‘ई- गवनेंस’ कहलाता है, जिसका लक्ष्य आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि व है कि राष्ट्रीय-गवनेंस कार्यक्रम अंतर्गत प्रारंभ में 31 सेवाएं शामिल की थीं। इस प्रकार की अवधारणा सुशासन की परिपाटी को भी सुसज्जित करती है। पंचायती राज व्यवस्था आम लोगों | की ताकत है और खास प्रकार की राजनीति से दूर है। यह ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं द्वारा स्वयं पर शासन किया जाता है। बीते तीन दशकों में पंचायतें बदली हैं। इन सब में एक प्रमुख बात यह रही है कि महिलाएं तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय हुई हैं। राज्य सरकारों का ऐसी संस्थाओं पर भरोसा बढ़ा है। गांवों में विकास को रफ्तार देने में इनकी भूमिका बढ़ी है।