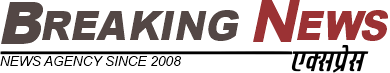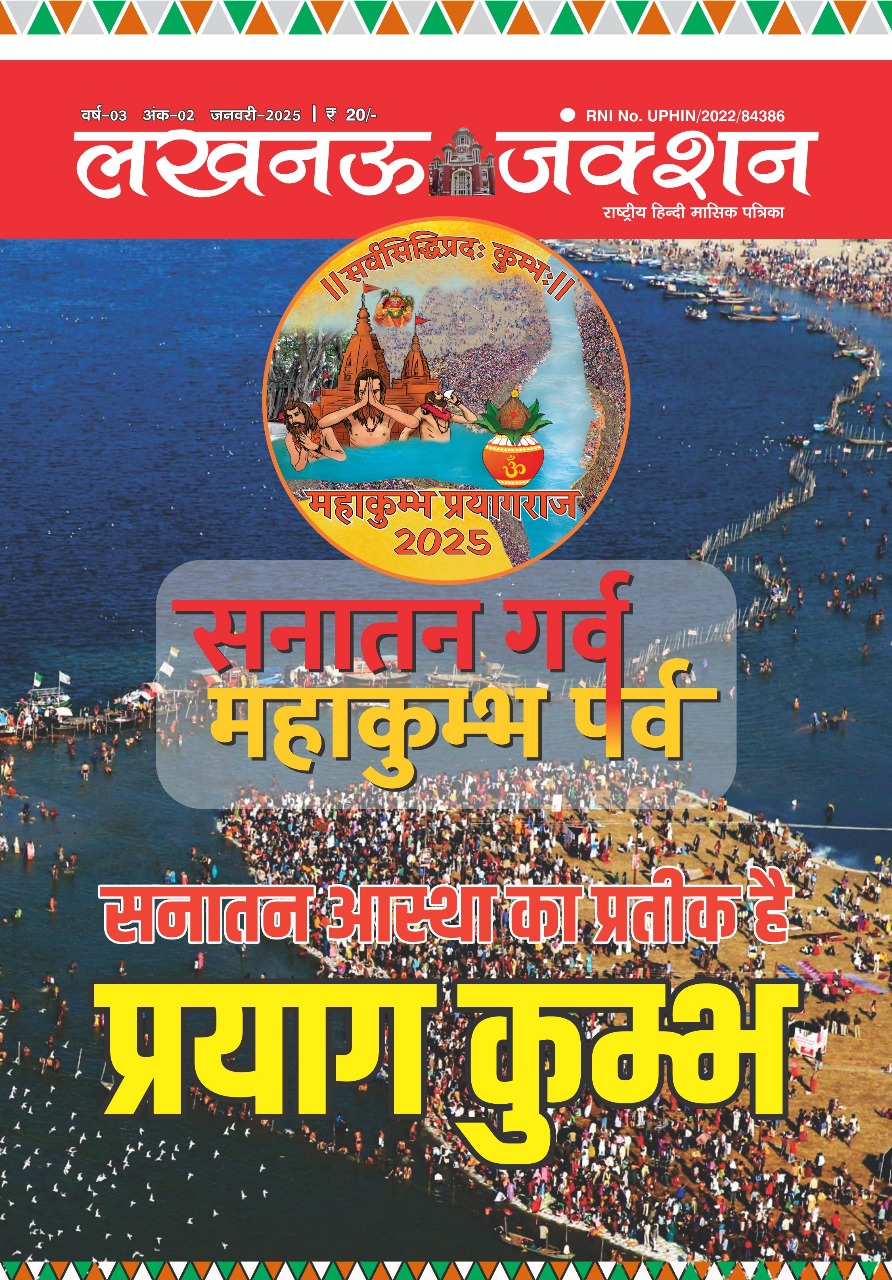नाम नहीं, काम की संस्कृति -विजय गर्ग
भारत बहुत प्राचीन देश है। यहां की सांस्कृतिक विविधता ही हमारी पहचान है। आजादी का शतकीय महोत्सव, जो हम वर्ष 2047 में मनाने वाले हैं, उसके लक्ष्य में भी यही इच्छा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखकर विश्वगुरु की भूमिका निभाए। वर्तमान सरकार की भी यह घोषणा है कि अपने देश में जिस विकास की नींव हम रख रहे हैं, उसका सुफल हजारों वर्षों तक मिलेगा तथा हमारी सांस्कृतिक गरिमा और भव्यता बनी रहेगी। बहुत-सी बातें हैं जिनके बल पर हम इस दावे को प्रमाणित करना चाहते हैं। भारत एक युवा देश है और इसकी आधी आबादी कार्यशील उम्र अवधि में है। इसलिए अगर यह आधी आबादी काम पर या राष्ट्र निर्माण में लग जाए तो भारत को दूसरे देशों से आगे निकलने में देर नहीं लगेगी। मगर, हमारी अर्थव्यवस्था के प्रशस्ति गायकों का यह मत है कि हम दुनिया के विभिन्न देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थ में पहुंच गए हैं और अब जरूरत है अर्थव्यवस्था में कुछ और करने की। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे।
अब देखना यह है कि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग क्या देश में काम की संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण रपट आई है, जिसमें विभिन्न देशों की मेहनत वृत्ति या काम करने की अवस्था का आकलन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में कम से कम आधी आबादी काम के बजाय आराम करना पसंद करती है, क्योंकि मुफ्तखोरी और अनुकंपा संस्कृति का चलन बढ़ रहा है। एक और बात सामने आई है कि भारत में बहुत सारे लोगों की मेहनत को श्रेय या
पारिश्रमिक ही नहीं मिलता है। जैसे महिलाएं इस देश की आबादी का करीब आधा हिस्सा हैं। इनमें से ज्यादातर की मेहनत को घर का सामान्य कामकाज ही समझा जाता है। इस काम के लिए उन्हें अलग से कोई नियत वेतन नहीं मिलता। ये महिलाएं दिनभर काम में व्यस्त रहने के बावजूद अपने लिए कोई अलग आर्थिक संबल प्राप्त नहीं कर पातीं।
इसमें संदेह नहीं कि आज भी जो बेकारी के आंकड़े सामने आते हैं, उनमें ग्रामीण बेरोजगारी के बाद शहरी बेरोजगारी में भी वास्तविक अर्थों में कोई कमी होती नजर नहीं आ रही। चाहे औपचारिक घोषणाओं में हम यह कहते रहें कि हमने हजारों खाली पद भर लिए हैं, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि हमने कितने खाली पद भरे, बल्कि देश की युवा संतति के कामकाज के लिए कितनी नई कार्य व्यवस्थाएं सृजित की गई। देश के वार्षिक बजट में के आय-व्यय ब्योरे में हम कितनी उन नई योजनाओं की घोषणा कर पाए, जिनमें युवा पीढ़ी को काम मिले। बेशक बजट में और इसके बाद नेताओं के भाषणों में यह कहा जाता है कि देश मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इनमें साधारण नागरिकों को रोजगार देने की क्षमता है। पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री ने भी एक वक्तव्य दिया कि देश में सहकारिता की भावना को विकसित किया जाएगा, ताकि अधिक से
अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन जब हम वास्तविकता का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि मध्यम और कुटीर उद्योगों के विकास में भी बड़े पूंजीपतियों के निवेश का प्रवेश हो गया है, क्योंकि, सरकार की नीति निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की है। सहकारिता आंदोलन के विकास के बारे में बहुत से औपचारिक बयान दिए जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि सहकारिता की भावना को
किसी भी समर्पित स्तर पर देश में अपनाया नहीं जा सका है। न तो कृषि और न ही उद्यम क्षेत्र में देश में नवउद्यमों की बहुत बात होती है। नवउद्यम वे उद्योग हैं, जिनमें नए निवेशकों को काम करने का अवसर मिलता है और नवाचार या नव अन्वेषण को प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन नवउद्यमों का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। धनी लोग जो बैंकिंग सहायता से इन उद्योगों में में सक्रिय योगदान दे सकते अदान दे सकते हैं, उनकी भागीदारी कम हो रही है। कृत्रिम मेधा और डिजिटल क्षेत्र के विकास के साथ- साथ अल्प पूंजी वाले निवेशकों का फीसद इसमें कम होता जा रहा है। उधर, शुल्क संघर्ष में विदेशी व्यापार इस तरह से करवट बदलता नजर आ रहा है कि लगता है भारत के निवेशकों को लागत पूरा न होने और निर्यात घटने के संशय से औद्योगिक सक्रियता कम करनी होगी। इसीलिए अब जो नए आंकड़े रेटिंग एजेंसी मूडीज की ओर से आए हैं, उनमें यह कहा गया है कि भारत की इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.5 फीसद से कम होकर छह फीसद तक रह सकती है। यह कोई संतोष की बात नहीं है कि हमारी विकास दर अभी भी दुनिया में सबसे अधिक है। देखना होगा कि जो पीढ़ी काम कर सकती हैं, क्या इस विकास दर ने उन्हें काम दिया? अगर आय और संपदा का समुचित बंटवारा हो जाता, तो निश्चय ही यह विकास दर बेरोजगारों को रोजगार देती।
आजकल लगता है कि देश में दावा संस्कृति या नाम संस्कृति का बोलबाला हो गया है। अभी सरकार की ओर से बयान आया कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। यह बयान तो पहले ही आ गया था कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। लेकिन आर्थिक सामर्थ्य का यह बड़प्पन क्या देश में काम करने वालों के लिए काम की संस्कृति पैदा रहा है? क्या ? क्या हमने देश ‘हर नौजवान के लिए उसकी योग्यता के अनुसार काम के अवसर सृजित किए हैं? जवाब है, नहीं यह बात सच है कि हमने किसी भी व्यक्ति को भूख से न मरने देने की गारंटी दे रखी रखी है। । इस गारंटी को पूरा करने के लिए हमने रियायती रेवड़ियां बांटना जारी रखा है। इसके लिए सभ्य नाम उदार संस्कृति हैं और आर्थिक नाम अनुकंपा । संस्कृति है। वर्ष 2029 तक हमने सस्ता खाद्यान्न प्रदान करने की नीति को बढ़ा ही दिया है। असर यह हुआ है कि नौजवानों का दबाव रोजगार खिड़कियों से हटकर रियायती अनाज बांटने वाली खिड़कियों की ओर हो गया है।
ज्यों-ज्यों चुनावी एजेंडों में नई अनुकंपा योजनाओं की घोषणा होती है, त्यों-त्यों भारत के दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिने जाने की संभावना मजबूत होती है, जो अपनी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटता है। मगर, अपने आप में क्या यह कार्य संस्कृति से हटना नहीं ? जापान और चीन ने जितनी तरक्की की है, वह इसीलिए संभव हो सका कि वहां काम की संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता है। हमारे यहां तो नाम संस्कृति कह लीजिए या रेकार्ड बनाने की संस्कृति कि हमने सबसे अधिक आबादी को रियायती अनाज दे दिया। ऐसे में जरूरी है कि काम की तलाश में विदेश जा रही हमारी युवा पीढ़ी को देश में ही राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए। मगर उसके लिए देश के नीति निर्माताओं को घोषणा संस्कृति से हटकर कार्य संस्कृति को लेकर प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और प्राथमिकताओं की तस्वीर को जरूरत के हिसाब से बदलना होगा।