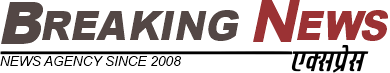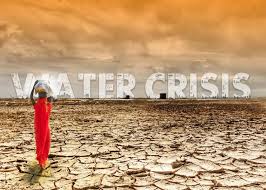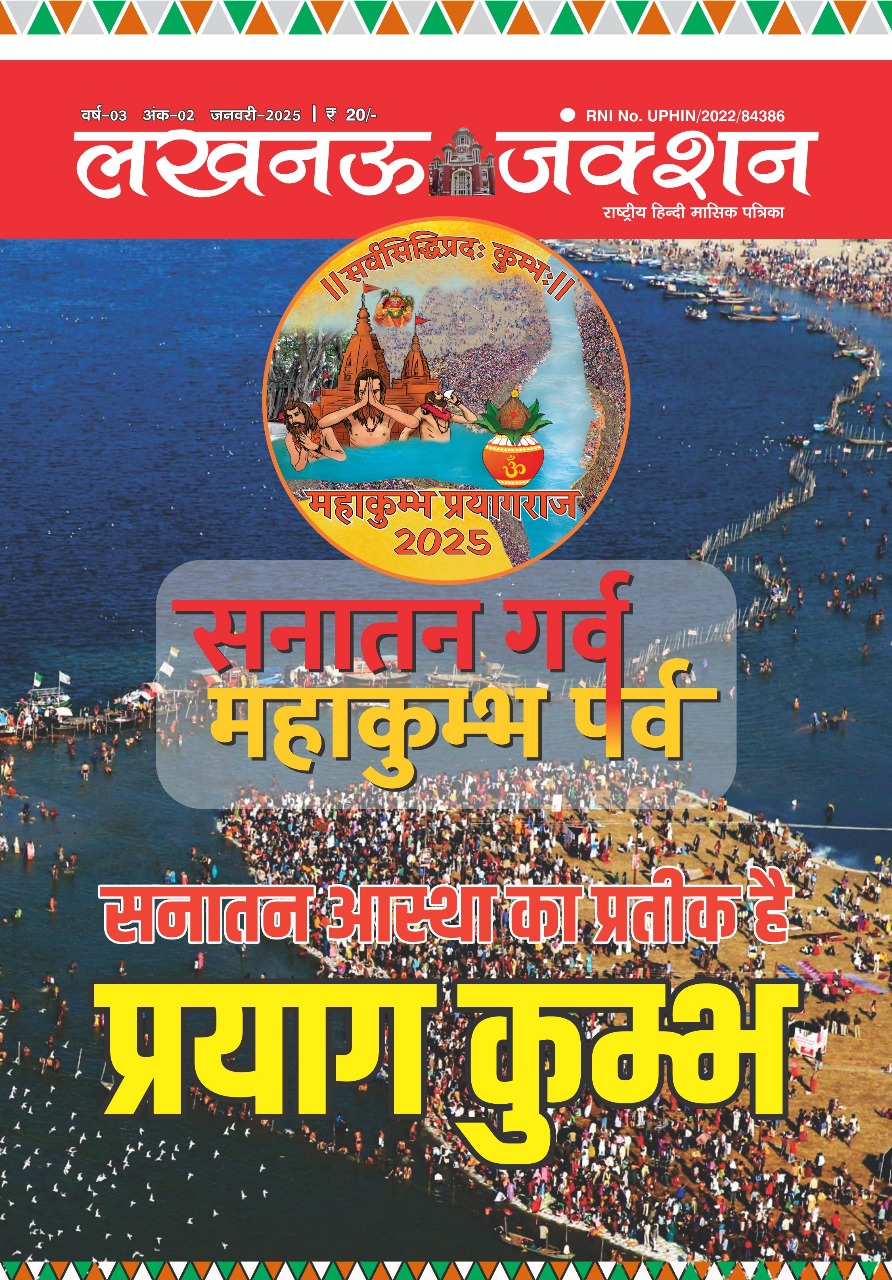भारत का लूमिंग वाटर क्राइसिस: स्कारसिटी से सस्टेनेबिलिटी तक
विजय गर्ग
सभी जीवित प्राणियों के जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है। पृथ्वी के महासागरों, समुद्रों, झीलों, नदियों और अन्य निकायों में लगभग 71 प्रतिशत पानी से ढके होने के बावजूद – केवल एक छोटा सा अंश ताजा और प्रयोग करने योग्य है। महासागर विशाल, खारे पानी के निरंतर विस्तार हैं, जबकि समुद्र, हालांकि छोटे और भूमि-संलग्न हैं, सीधे मानव आजीविका से जुड़े हुए हैं। हालांकि, मीठे पानी से पृथ्वी के कुल पानी का सिर्फ 2.5 प्रतिशत बनता है, जिसमें से 98.8 प्रतिशत बर्फ की टोपी और भूमिगत जलभृतों में बंद हो जाते हैं। केवल 0.3 प्रतिशत नदियों, झीलों और वायुमंडल में आसानी से सुलभ है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, वनों की कटाई, वायु प्रदूषण और मृदा क्षरण के तेज खतरे के साथ, पृथ्वी पर जीवन के भविष्य का निर्धारण करने में मीठे पानी की उपलब्धता और प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा। भारत जैसे देश के लिए चुनौती और भी गंभीर है. दुनिया के केवल 2.4 प्रतिशत भू-भाग पर 145 करोड़ लोगों की मेजबानी करते हुए, भारत का जल संकट पहले से ही स्वास्थ्य, कृषि और शहरी बुनियादी ढांचे पर भारी पड़ रहा है।
भारत में दुनिया के मीठे पानी के संसाधनों का लगभग 4 प्रतिशत है और सालाना लगभग 115 इंच (या 2900 मिमी) वर्षा होती है। हालांकि, यह वर्षा अत्यधिक असमान है – दोनों स्थानिक और मौसमी रूप से – जून और सितंबर के बीच लगभग 75 प्रतिशत गिरने के साथ। इसके अलावा, भारत की अधिकांश घरेलू जरूरतें (85 प्रतिशत) और कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (70 प्रतिशत) भूजल पर निर्भर करती हैं। यह एक्विफर्स की स्थिरता को बिल्कुल महत्वपूर्ण बनाता है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, भारत को सालाना लगभग 3950 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) वर्षा होती है। लेकिन वाष्पीकरण और अन्य नुकसान के लिए लेखांकन के बाद, केवल 1999 बीसीएम उपलब्ध है, और सिर्फ 1126 बीसीएम उपयोग करने योग्य है। दुर्भाग्य से, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए हमारी कुल पानी की मांग सालाना 2800 से 3000 बीसीएम के बीच है – उपलब्ध आपूर्ति से कहीं अधिक।
भारत की प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है – 1951 में 5100 घन मीटर से 2021 में 1545 घन मीटर तक – 1700 घन मीटर की जल तनाव सीमा को पार करना। इसमें और गिरावट आने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भूजल की गंभीर अधिकता देखी जा रही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार, 17 प्रतिशत ब्लॉक पहले से ही निकाले गए हैं। इसके अलावा, बाढ़ सिंचाई जैसी अक्षम कृषि पद्धतियां व्यापक हैं, जबकि ड्रिप सिंचाई जैसे आधुनिक तरीके केवल 2.3 प्रतिशत खेती की गई भूमि को कवर करते हैं। कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देने वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) में अभी भी प्रभाव के मामले में लंबा रास्ता तय करना है।
शहरी भारत भी दबाव में है। चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर गर्मियों के दौरान पानी की तीव्र कमी से पीड़ित हैं, मोटे तौर पर अनियोजित शहरी विस्तार के कारण। संकट को जोड़ना जल निकायों का बढ़ता प्रदूषण है, जिससे स्वच्छ, प्रयोग करने योग्य पानी की उपलब्धता को और कम किया जा सकता है।
इन बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए, एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्रीय जल संरक्षण रणनीति समय की आवश्यकता है। इस रणनीति को हमारी जलवायु परिवर्तन शमन योजनाओं के साथ संरेखित करना चाहिए और क्षेत्रीय विषमताओं को संबोधित करना चाहिए – जैसे कि पंजाब और हरियाणा में भूजल की कमी, और तमिलनाडु और कर्नाटक में सूखाग्रस्त स्थितियां। जलवायु परिवर्तन वर्षा पैटर्न में बदलाव और बाढ़, सूखे, भूस्खलन और ग्लेशियर से संबंधित आपदाओं को ट्रिगर करके समस्या को बढ़ा रहा है। इसलिए, एक व्यापक जल प्रबंधन चार्टर की आवश्यकता होती है – एक जो हरे पानी (मिट्टी में संग्रहीत वर्षा जल), नीले पानी (सतह मीठे पानी), और ग्रे पानी (घरों से अपशिष्ट जल) को संबोधित करता है – गांव के स्तर से शुरू होता है और राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करता है। सकारात्मक घटनाक्रम के बीच, 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन, बाहर खड़ा है। उस समय, 18 करोड़ में से केवल 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास साफ नल के पानी तक पहुंच थी। 2025 की शुरुआत में, यह संख्या बढ़कर 15.44 करोड़ हो गई है – लगभग 80 प्रतिशत कवरेज। इस पहल ने जलजनित बीमारियों को कम करके अनगिनत लोगों की जान बचाई है और निवारक स्वास्थ्य सेवा के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है।
हालांकि, राष्ट्रीय जल मिशन में उल्लेख के बावजूद, पॉलिसी स्तर पर ध्यान अभी भी नीले पानी के प्रबंधन की ओर बहुत अधिक है, हरे पानी पर थोड़ा ध्यान देने के साथ। भारत को अब एक परिदृश्य की आवश्यकता है – एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के लिए स्तर का दृष्टिकोण। विभिन्न विभागों को साइलो में काम करना बंद करना चाहिए और स्थायी जल संरक्षण के प्रयासों का समन्वय करना चाहिए। एक तत्काल समाधान वन, पंचायत और सामुदायिक भूमि पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण हो सकता है। इस तरह के बुनियादी ढांचे से वर्षा जल पर कब्जा करने, जलभृत पुनर्भरण और जलवायु लचीलापन में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, राजस्थान में, जोहड्स – समुदायों द्वारा निर्मित छोटे मिट्टी के बांध – हरे जल संरक्षण में प्रभावी साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कुंडी भंडारा जैसे ऐतिहासिक इंजीनियरिंग चमत्कार, अब्दुल रहीम खान-ए-खाना द्वारा मुगल युग के दौरान निर्मित, प्रेरणा के रूप में भी काम करते हैं। इस प्रणाली ने भूजल को इकट्ठा करने और परिवहन करने के लिए भूमिगत सुरंगों और घुसपैठ दीर्घाओं का उपयोग किया, अपने समय से पहले स्वदेशी नवाचार सदियों का प्रदर्शन किया। अंत में जल संकट एक दबाव वास्तविकता है। समाधान मौजूद हैं – विज्ञान, नीति और परंपरा में। अब जो आवश्यक है वह एकीकृत, दूरदर्शी कार्रवाई और स्थायी जल उपयोग के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। जैसा कि इतिहास और आधुनिक उदाहरण दोनों दिखाते हैं, नवाचार, एकीकरण और सामुदायिक भागीदारी भारत के जल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब