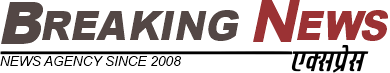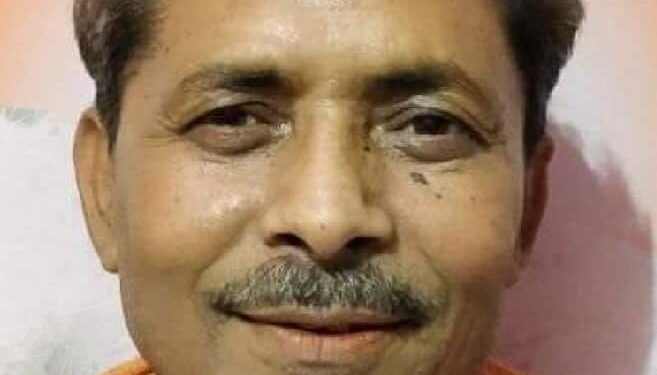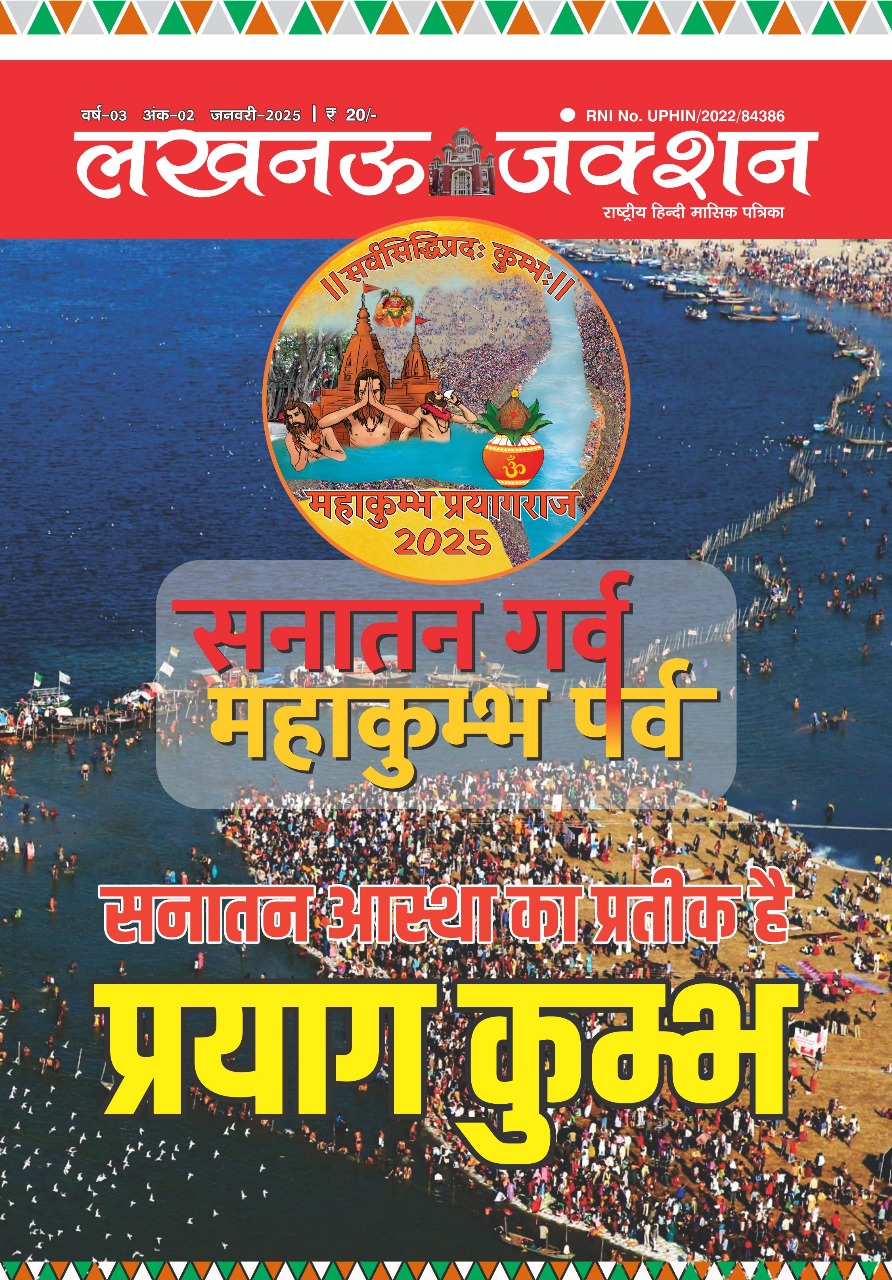झनकार नाथ शुक्ल( Breaking news express )
प्रेम को आद्यंतहीन आध्यात्मिक यात्रा की मान्यता देने वाली विदुषी लेखिका डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित ने अपनी पुस्तक “प्रेमदूत” के संग मरमरी 136 पृष्ठों को 16 आलेखों की मनमोहक रंगोलियों, सुंदरतम अल्पनाओं से सजाने में अथक परिश्रम किया है। ऋग्वेद से लेकर आज तक के अनेक अपेक्षित ग्रन्थों का अध्ययन किया है। इन आलेखों की मोहक अल्पनाओं पर प्रसन्न होकर प्रोफेसर, पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह के हृदय से निकले “आशीर्वचन” से इस कृतिका शुभारंभ है। डॉ गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर ने अपने “भारतीय साहित्य में प्रेमदूत” आलेख में पुस्तक के संपूर्ण कलेवर की जो झांकी प्रस्तुत की है, वह पुस्तक के प्रति पाठक को जिज्ञासु बनाकर पुस्तक की महत्ता को प्रतिपादित करती है। डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित ने अपने “मन की बात” आलेख में अपनी प्रथम कृति “प्रेमदूत” लिखने के प्रेरक तत्वों में वेदों, उपनिषदों तथा कवि कुलगुरू कालिदास के संपूर्ण साहित्य के काव्य सौंदर्य को तथा विशेष रूप से “मेघदूतम” का उल्लेख किया है। मेघदूतम के वर्ण्य विषय और भाव संपदा को लेखिका ने मेघ की भांति दूत भेजने संबंधी साहित्य के खोज की प्रेरणा प्रदान की। इसी खोजबीन की सुपर्णिति का सुपरिणाम ही प्रेमदूत है। मन की बात में लेखिका ने सभी सहयोगियों सभी प्रेरणा स्रोतों का आभार व्यक्त किया है। सभी संदर्भ ग्रन्थों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। मन की बात में लेखिका ने वेदों, उपनिषदों, कालिदास के अन्य ग्रन्थों को पढ़ने की जिज्ञासा भी जगाई है तथा श्रम साध्य प्रेमदूत पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित करने की योजना में सफल सिद्ध हुई है। प्रोफेसर भरत प्रसाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग प्रेमदूत की भूमिका लेखन में कालिदास की अमर कृति मेघदूत की भित्ति पर कबीर के ढाई अक्षर प्रेम की लकीर का स्मरण करते हुए कविवर बिहारी लाल के प्रेम संकेतक तक डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित की प्रेमदूत यात्रा की सराहना की है। भावी समय में डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित बदलते स्वर में यह यात्रा जारी रखेंगी यह आस भी संजोई है। “प्रेमदूत का परिचय” प्रेमदूत कृति का प्रथम अनुशीलनात्मक आलेख है। प्रेम आज तक अपरिभाषित है और आगे भी अपरिभाषित ही रहेगा । जहां सारे शब्दों के अर्थ विलीन हो जाते हैं वहीं से प्रेम जन्म लेता है। प्रेम शब्दातीत है। प्रेम अनुभव गम्य है, वर्णन की वस्तु नहीं। प्रेम के संबंध में लेखिका की यही मान्यताएं हैं। कालिदास की अमर कृति मेघदूतम में प्रेमदूत के रूप में वर्णित मेघदूत के विलक्षण काव्य सौंदर्य ने उन्हें ऋग्वेद, बाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत श्रीरामचरितमानस, मानस पीयूष, अष्टछाप के कवि, नैषधीयचरित , अभिनव मेघदूतम, ढोला मारू की प्रेम कथा, पद्मावत आदि ग्रन्थों में प्रेमदूत प्रेम संदेश ढूंढने के लिए, अनुशीलन करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय वाङ्मय में प्रथम संदेश वाहिका इंद्र की देवदूती देवसुनी शर्मा हैं।यह आख्यान ऋग्वेद के दशम मंडल में वर्णित है। देव सुनी शर्मा बादलों की गड़गडड़ाहट की धुन से पणियों को इंद्र का संदेश देती है। भारतीय साहित्य के दूसरे सबसे बड़े संदेशवाहक ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद मुनि हैं। श्री नारद जी एक ऐसे संवाददाता हैं जो सुरों असुरों के पास जाकर अपेक्षित अनापेक्षित सूचनायें पहुंचाते रहते हैं। श्री नारद जी को प्रथम पत्रकार के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्री नारद जी को तीन घड़ी से अधिक एक स्थान पर न रुकने का श्राप है। श्री नारद जी ने इस श्राप को संवादों के आदान-प्रदान के रूप में प्रयोग करके वरदान में बदल लिया है । कृति का द्वितीय आलेख “रामदूत हनुमान” है। संदर्भ ग्रंथ बाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड है। सुंदरकांड में राम कथा नहीं है इस कांड में राम भक्त हनुमान की कथा और माता सीता की व्यथा है। भगवान राम समेकित रूप से श्री हनुमान जी को अपना दूत और प्रेमदूत बनाकर सीता की खोज के लिए भेजते हैं। प्रमाणिक प्रेम प्रदर्शन के लिए अपनी अंगूठी भी देते हैं । श्री हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचकर अंगूठी देकर भगवान राम का संदेश कहते हैं।
मो मनु रहति सदा तोहि पाहीं।
जानु प्रीति रस इतनेहि माही।

लंका दहन के पश्चात मारुति नंदन के प्रति सीता विश्वस्त हो जाती हैं और अपना प्रेम समर्पण अपनी चूड़ामणि देकर अपने स्वामी भगवान राम को भेजती हैं। श्री राम के पूछने पर श्री हनुमान जी सीता जी की स्थिति बताते हैं –
नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट।
लोचन निज़ पद जंत्रित जाहि प्राण केहि बाट।।
कृति के तृतीय आलेख में “कृष्णदूत उद्धव” को लिखने में लेखिका ने जिन रचनाकारों के संदर्भ ग्रन्थों का अनुशीलन किया उनमें श्रीमद् भागवत, सूरदास का सूरसागर, नंददास का भंवर गीत, तुलसीदास की श्री कृष्ण गीतावली, मतिराम, पद्माकर, घनानंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उल्लेख भी किया है , उन्हें उद्धृत भी किया है। इन सभी रचनाकारों ने ब्रज की गोपियों को समझने के लिए मथुरा वासी हो गए भगवान कृष्ण की ओर से उद्धव को संदेश वाहक बनाकर भेजा है। गोपियों को समझाने बृज पहुंचे उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद हुआ उसे भ्रमर गीत नाम से अभिहित किया गया है ।
सभी रचनाकारों के कृष्ण उद्धव और गोपियां अद्भुत है। गोपियों और उद्धव के पारस्परिक प्रश्नोत्तरों की विषय वस्तु पर रचनाकारों ने रचनायें की हैं। महात्मा सूरदास ने विस्तृत रूप से इस संवाद को अपने पदों में गाया है। लेखिका द्वारा कुछ उदाहरण प्रस्तुत है
“ऊधो मन न भये दस बीस।
सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश ।।
सूरदास
“आए हउ सिखावन को योग मथुरा तै तोपि,ऊधौ ए वियोग के वचन बतराओ ना।
एक मनमोहन तो बसिकै उजारयौ मोहि ,हिय में अनेक मनमोहन बसावो ना।।
जगन्नाथ दास रत्नाकर
ऊधौ जू सूधौ गहौ वह मारग ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। एक जो होय तौ ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहां भांग परी है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र कृति का चौथा आलेख रुक्मिणी का संदेश है रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी वह अपने को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। उनका भाई बलात् उनका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण द्वारा कृष्ण को संदेश भेजा। मैं कुल रीति के अनुसार अमुक् तिथि को गिरजा दर्शन के लिए जाऊंगी, वहीं आकर मेरा वरण करो अन्यथा में प्राणों का परित्याग कर दूंगी। श्री कृष्ण ब्राह्मण द्वारा संदेश पाकर आए और निश्चित समय पर रुक्मिणी जी का वरण किया। इस आलेख का संदर्भ ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। कृति के पांचवें आलेख “नल दमयंती की कथा” का मूल संदर्भ ग्रंथ श्री वेदव्यास कृत विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ महाभारत है। श्री हर्ष रचित नैषधीय चरित में भी इस कथा को अपना विषय बनाया गया है। इस कथा में हंसों ने प्रेमदूतों का काम किया है ।अद्वितीय रूप गुण शील संपन्न राजा नल के संबंध में प्रेम दूत बनकर दमयंती को हंस बताते हैं, हंस ही दमयंती के विषय में राजा नल को बताते हैं। दमयंती की आश्चर्यजनक सौंदर्य लिप्सा में देवता भी सम्मिलित होते हैं। दोनों के प्रेम में बाधक बनते हैं। और भी बाधायें आती हैं ।नल दमयंती का सच्चा प्रेम सभी बाधावों को पार कर एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। कृति का छठवां आलेख मेघदूत है। कालिदास के मेघदूतम को ही लेखिका ने प्रेमदूत पुस्तक का आधार स्वीकार किया है। मेघदूतम के सौंदर्य बोध व प्रकृति वर्णन पर लेखिका बहुत मंत्र मुग्ध है। मेघदूतम का काव्य सौंदर्य अद्भुत है ही। उस पर मुग्ध हुए बिना कौन रह सकता है। “मेघदूतम से प्रेरित साहित्यकारों की अन्य रचनाएं” इस कृति का सातवां आलेख है ।लेखिका का मानना है कि मेघदूतम ने ही उसे प्रेमदूत लिखने की प्रेरणा दी । महान कवि रवींद्र नाथ ठाकुर, हरिवंश राय बच्चन ,गुलाब खंडेलवाल आदि सिद्धि रचनाकारों ने मेघदूत से प्रभावित होकर रचनायें लिखकर मेघदूत गीति काव्य के प्रति इस प्रकार श्रद्धा व्यक्त की है जैसे कोई गंगा में खड़ा होकर गंगा को अर्घ्य देता है। लेखिका ने अपने आठवें आलेख में राजस्थान की “केहर कंवल की कहानी” को इस पुस्तक में जोड़ा है ।नवें आलेख में राजस्थान की “ढोला मारू की कथा” को अपनी प्रेमदूत पुस्तक में स्थान दिया है। इस कृति का दसवां आलेख “पद्मावत नागमती” है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित अवधी भाषा के इस ग्रंथ की शब्द संपदा भाव संपदा बड़ी जबरदस्त है। पद्मावती नागमती तथा राजा रतन सेन के बीच संयोग वियोग के झूले में झूलते गहन प्रेम संदेशों का वाहक हीरामन तोता बनता है। नागमती अपनी विरह व्यथा अपने प्रिय तक पहुंचाने के लिए पवन दूत को भी अपना प्रेम दूत बनाती हैं। इस कृति का 11वां आलेख “मीराबाई” है मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति, स्वामी मानती है। उन्हीं की आराधना में लगी रहती हैं। साधु संतों की संगत करती हैं ।इन कार्यों की समाज में स्वीकार्यता नहीं है। उन्हें तमाम प्रताडड़नाओं को सहन करना पड़ता है। परेशान होकर सुखपाल नामक ब्राह्मण द्वारा गोस्वामी तुलसीदास को मार्गदर्शन हेतु संदेश भेजती हैं। गोस्वामी जी उत्तर भेजते हैं।
“जाके प्रिय नाम राम वैदेही।
तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही।
कृति का 12 वां आलेख “हाड़ी रानी की कहानी” है। राजस्थान की बलिदानी धरती के दो बलिदान बहुत चमकदार हैं। विश्व के इतिहास में केवल राजस्थान में ही है। पहला पन्नाधाय का त्याग और दूसरा हाड़ी रानी का बलिदान। दोनों घटनाएं ऐतिहासिक हैं मेवाड़ के राजा जयसिंह के बुलावे पर चूड़ावत सरदार सद्य व्याहता पत्नी हाड़ी रानी को छोड़कर रण क्षेत्र के लिए निकल पड़ते हैं। राण क्षेत्र से ही एक सैनिक को रानी के पास निशानी के लिए भेजते हैं। हाड़ी रानी अपने स्वामी की अपने ऊपर इस अनुरक्ति को भांप कर यह सोचकर कि कहीं मेरे स्वामी अपने दायित्व का निर्वाह करने से च्युत न हो जाएं तत्काल उस सैनिक को अपनी अंतिम निशानी के रूप में शीश काटकर स्वर्ण थल में रख दिया। इन दोनों घटनाओं को महान साहित्यकारों ने अपना विषय बनाया है। कृति का 13वां आलेख “बिहारी लाल के प्रेम संकेतक” है। बिहारी सतसई बिहारी लाल की अद्भुत कृति है। लेखिका द्वारा उधृत एक संकेतक दृष्टव्य है ।
कर लइ चूमि चढ़ाई सिर, उर लगाइ भुज भेंटि ।
लहि पाती पिय की लखति बांचति धरति समेटि। “
कृति के 14 वें आलेख में लेखिका ने “नीरज की पाती” को नीरज के रचनात्मक सौंदर्य बोध का उल्लेख करके “मानव होना भाग्य है कबि होना सौभाग्य” कहकर स्थान दिया है।
15 वें आलेख “उपसंहार” में लेखिका ने शोधपरक अपनी कृति प्रेमदूत को मौलिक सोंच मानकर संतुष्टि जताई है। 16 वें में संदर्भ ग्रंथों की सूची देकर अमर कृतियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है ।
कृति का शीर्षक “प्रेमदूत” उपयुक्त है। भाषा शिल्प विषय के अनुकूल है इस कृति को मैंने एक बैठक में पढ़ा मेरी दृष्टि में पुस्तक की यह भी एक बड़ी सफलता है। पुस्तक का संपूर्ण कलेवर सभी आख्यान सभी कथाएं देर सबेर पढ़ी हुई होने के बावजूद कृति को पढ़ने में आनंद की अनुभूति लेखिका के आकर्षक लेखन का सटीक परिणाम लगा। पुस्तक चर्चा की सफलता पाठकों में पुस्तक पढ़ने की जिज्ञासा की सीमा ही तय करेगी संप्रति इतना ही ।