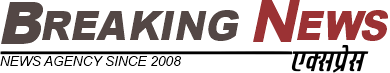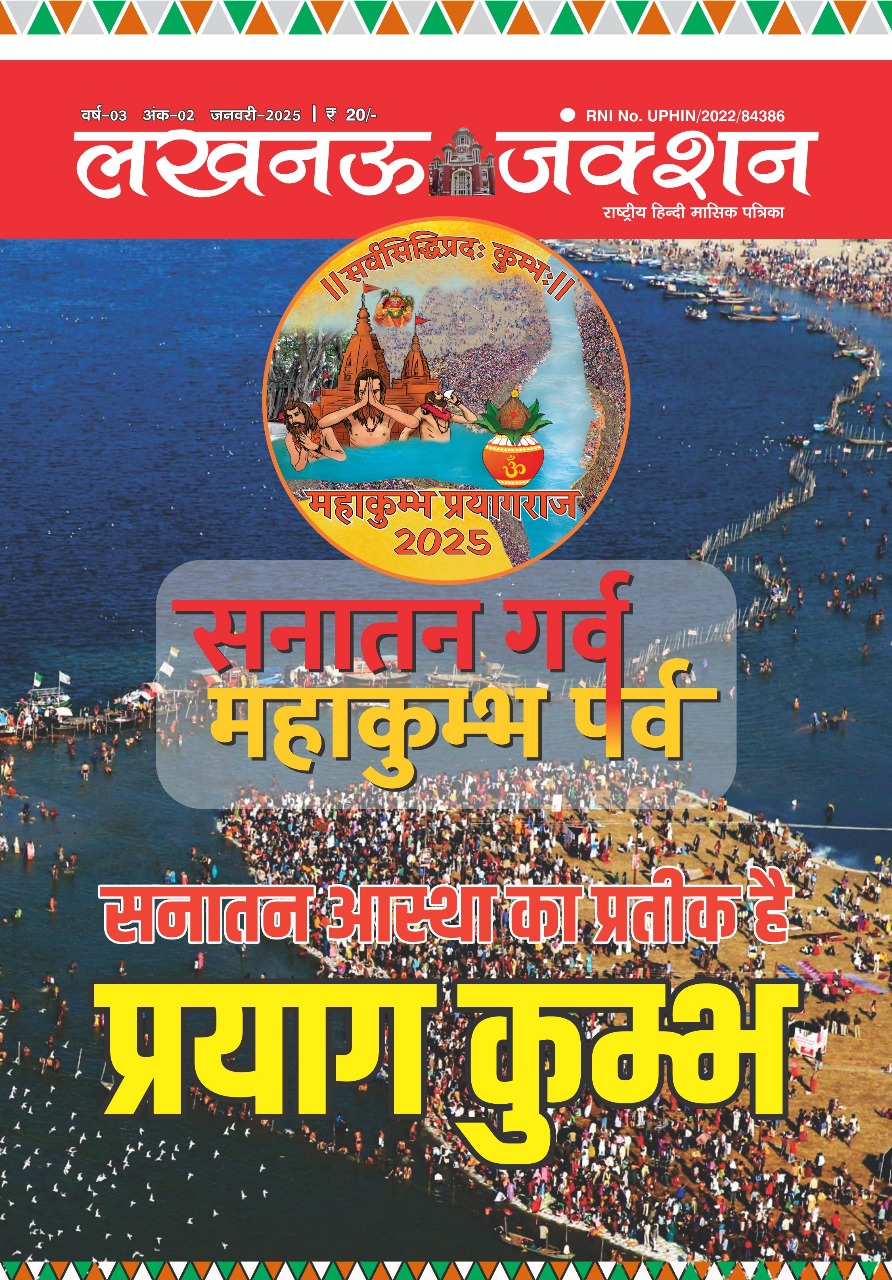इलेक्शन कमीशन : पब्लिक का भरोसा या पॉलिटिक्स का प्रेशर”
जनता की आँखों में भरोसा, आयोग के कंधों पर जिम्मेदारी"
भारतीय चुनाव आयोग कभी लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव माना जाता था। लेकिन हालिया वर्षों में उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं—मतदाता सूची से नाम गायब होना, मतदान प्रतिशत में देरी और असंगति, ईवीएम-वीवीपैट मिलान की सीमाएँ, तथा आयुक्तों की नियुक्ति पर राजनीतिक प्रभाव। आचार संहिता के लागू होने में भी दोहरा मापदंड दिखाई देता है। सबसे बड़ा संकट यह है कि जनता का भरोसा डगमगाने लगा है। लोकतंत्र का अस्तित्व केवल मशीनों पर नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास पर टिका है। आयोग के लिए यही भरोसा बचाना सबसे बड़ी चुनौती है।
– डॉ. प्रियंका सौरभ
डॉ. प्रियंका सौरभ
भारतीय चुनाव आयोग कभी लोकतंत्र का सबसे विश्वसनीय प्रहरी माना जाता था। पर हालिया विवादों ने उसकी साख पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं—मतदाता सूची से नाम गायब होना, मतदान प्रतिशत की पारदर्शिता पर संदेह, और नियुक्तियों की प्रक्रिया पर उठते सवाल। चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब नियम बनाने या नोटिस भेजने की नहीं, बल्कि जनता के भरोसे को लौटाने की है। क्योंकि लोकतंत्र केवल वोटिंग मशीनों पर नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास पर चलता है। अगर विश्वास डगमगाया, तो चुनाव सिर्फ रस्म रह जाएंगे और लोकतंत्र अपने असली मायने खो देगा।
लोकतंत्र एक खेल है। खेल का मैदान जनता है, खिलाड़ी राजनीतिक दल हैं और रेफरी चुनाव आयोग। सवाल यह है कि जब रेफरी ही किसी एक टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतर आए तो खेल कितना निष्पक्ष रह जाएगा? हाल के दिनों में यही शंका बार-बार उठ रही है।
मतदाता सूची से नाम हटाने का मामला मानो एक नया सरकारी फैशन बन गया हो। वोटर घर बैठे सोचता है कि लोकतंत्र में उसका अस्तित्व है, लेकिन जब मतदान वाले दिन बूथ पर जाता है तो पता चलता है कि वह तो पहले ही “गायब” कर दिया गया है। जैसे कोई जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है, वैसे ही चुनाव आयोग नाम काटने की कला दिखा देता है। और जब आप शिकायत करने जाते हैं तो कहा जाता है—”जी शपथपत्र भरिए, गवाही दीजिए, साबित करिए कि आप जीवित हैं।” यानी इस देश में नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत अब यह नहीं कि आप साँस ले रहे हैं, बल्कि यह है कि आयोग ने आपके नाम पर पेंसिल से टिक लगाई है।
चुनाव आयोग की पारदर्शिता का हाल वैसा ही है जैसे दूल्हे की घोड़ी पर रखा हुआ दर्पण—सबको दिखता है, लेकिन पास जाते ही धुंधला हो जाता है। मतदान प्रतिशत का ऐलान भी किसी बॉलीवुड फिल्म के ट्रेलर जैसा है—पहले झलक दिखा दी, फिर कई दिन बाद असली आंकड़ा आया, और कभी-कभी तो दूसरा ट्रेलर पहले से लंबा निकल आया। जनता पूछती है कि जब बूथ पर वोट तुरंत गिन लिया जाता है, तो फिर प्रतिशत बताने में हफ्ता क्यों लगता है? आयोग का जवाब होता है—”हमारे ऐप पर सब था।” पर जनता सोचती है, जब शादी का कार्ड छपने से पहले सोशल मीडिया पर फोटो लाइव हो जाती है तो मतगणना का डेटा क्यों लटक जाता है?
अब आइए ईवीएम और वीवीपैट पर। आयोग का तर्क है कि मशीनें बिल्कुल सुरक्षित हैं। जनता कहती है—”हमें भी भरोसा है, पर पर्ची दिखा दीजिए।” आयोग कहता है—”पाँच बूथ काफी हैं।” यह वैसा ही है जैसे कोई दुकानदार हर सौ किलो आटे में से सिर्फ पाँच दाने तौलकर कह दे—”लो, साबुत निकले, अब बाकी पर भरोसा कर लो।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौ प्रतिशत मिलान जरूरी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में भरोसा केवल मशीन से नहीं आता, भरोसा जनता की आँखों से आता है। अगर जनता देखना चाहती है तो दिखाइए, आखिर छुपाना किस बात का है?
आयुक्तों की नियुक्ति का हाल और भी मज़ेदार है। पहले कहा जाता था कि यह नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर एक नया कानून आया और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही बाहर कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक मंत्री मिलकर तय करेंगे कि आयोग में कौन बैठेगा। यानी परीक्षा की कॉपी जाँचने वाला मास्टर खुद ही अपने पसंदीदा परीक्षार्थी को पास कराएगा। क्या ही निष्पक्षता है! विपक्ष के नेता की मौजूदगी बस औपचारिक है, वैसे ही जैसे शादी में बारात में आया कोई दूर का चाचा—बस दिखावे के लिए बैठा है, बाकी सारा खेल बड़े-बड़े काका निपटा लेते हैं।
आचार संहिता लागू करने में भी आयोग की अपनी “दृष्टि” है। कोई नेता ज़रा सी टिप्पणी कर दे तो नोटिस झट से चला जाता है। लेकिन वही बात अगर सत्ता पक्ष का नेता कर दे तो आयोग पहले गहरी ध्यान-स्थिति में चला जाता है, फिर योग निद्रा में और अंततः भूलने की बीमारी में। जनता कहती है कि आयोग सब पर बराबर डंडा चलाए, पर आयोग लगता है जैसे किसी शादी में नाचते हुए डीजे पर डंडा तभी चले जब वह पड़ोसी मोहल्ले का हो, घर के बाराती तो चाहे पटाखा फोड़ें, चाहे लाउडस्पीकर बजाएँ, सब मान्य है।
चुनाव चिन्ह और पार्टी विभाजन पर फैसले भी गजब के होते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के मामले में आयोग के निर्णय ऐसे लगे मानो पहले से पटकथा लिखी जा चुकी हो। जनता ने तंज कसा कि आयोग अब चुनाव का नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों का “संपत्ति-विभाजन अधिकारी” बन गया है। किसे पार्टी का नाम मिलेगा, किसे चुनाव चिन्ह—यह सब वैसे तय हुआ जैसे परिवार की जायदाद बंटती है। फर्क बस इतना कि अदालत की जगह अब आयोग बैठा है और फैसला किसके पक्ष में जाएगा, यह जनता पहले से जान लेती है।
असल संकट यह नहीं कि आयोग गलत कर रहा है या सही। असल संकट यह है कि जनता अब मानने लगी है कि आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। लोकतंत्र में धारणा ही सबसे बड़ी हकीकत होती है। अगर जनता को यकीन हो जाए कि वोट डालना महज औपचारिकता है, तो वह लोकतंत्र का उत्सव छोड़ कर अपने कमरे में क्रिकेट मैच देखने लग जाएगी। और अगर वोट डालने वाली कतारें छोटी होने लगीं तो लोकतंत्र की नींव खुद-ब-खुद हिल जाएगी।
सुधार की बातें खूब होती हैं, लेकिन असलियत यह है कि सुधार की ज़रूरत आयोग से ज्यादा उसकी सोच में है। मतदाता सूची से नाम हटाना अगर जरूरी है तो उसे दोहरी पुष्टि से कीजिए। मतदान प्रतिशत अगर तय समय में घोषित किया जा सकता है तो नियम बना दीजिए। ईवीएम सुरक्षित हैं तो पर्ची दिखाने से डर क्यों? नियुक्तियाँ अगर निष्पक्ष हैं तो न्यायपालिका को बाहर क्यों किया? आचार संहिता अगर सब पर लागू होती है तो नोटिस का रंग सत्ता के हिसाब से क्यों बदल जाता है?
लोकतंत्र एक जादुई शब्द है। यह तभी तक चमकता है जब तक जनता का भरोसा कायम रहता है। भरोसा टूटा तो लोकतंत्र का दीपक भी बुझ जाएगा। चुनाव आयोग के लिए यह समय है कि वह अपनी छवि बचाए। क्योंकि संस्थाएँ अपनी शक्ति सत्ता से नहीं, जनता से लेती हैं। सत्ता अस्थायी है, लेकिन जनता स्थायी है। आयोग यदि जनता का विश्वास खो देगा तो वह संवैधानिक ढांचे में केवल एक मुहर बनकर रह जाएगा।
आज आयोग के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है—क्या वह सचमुच लोकतंत्र का रेफरी है या सत्ता का बारातबाज़? रेफरी अगर सीटी सही समय पर नहीं बजाएगा तो खेल मैदान में ही तय नहीं होगा, बल्कि इतिहास में तय होगा। और इतिहास उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करता जिन्होंने लोकतंत्र की पवित्रता को दांव पर लगाया।