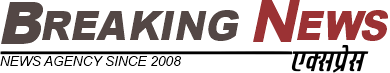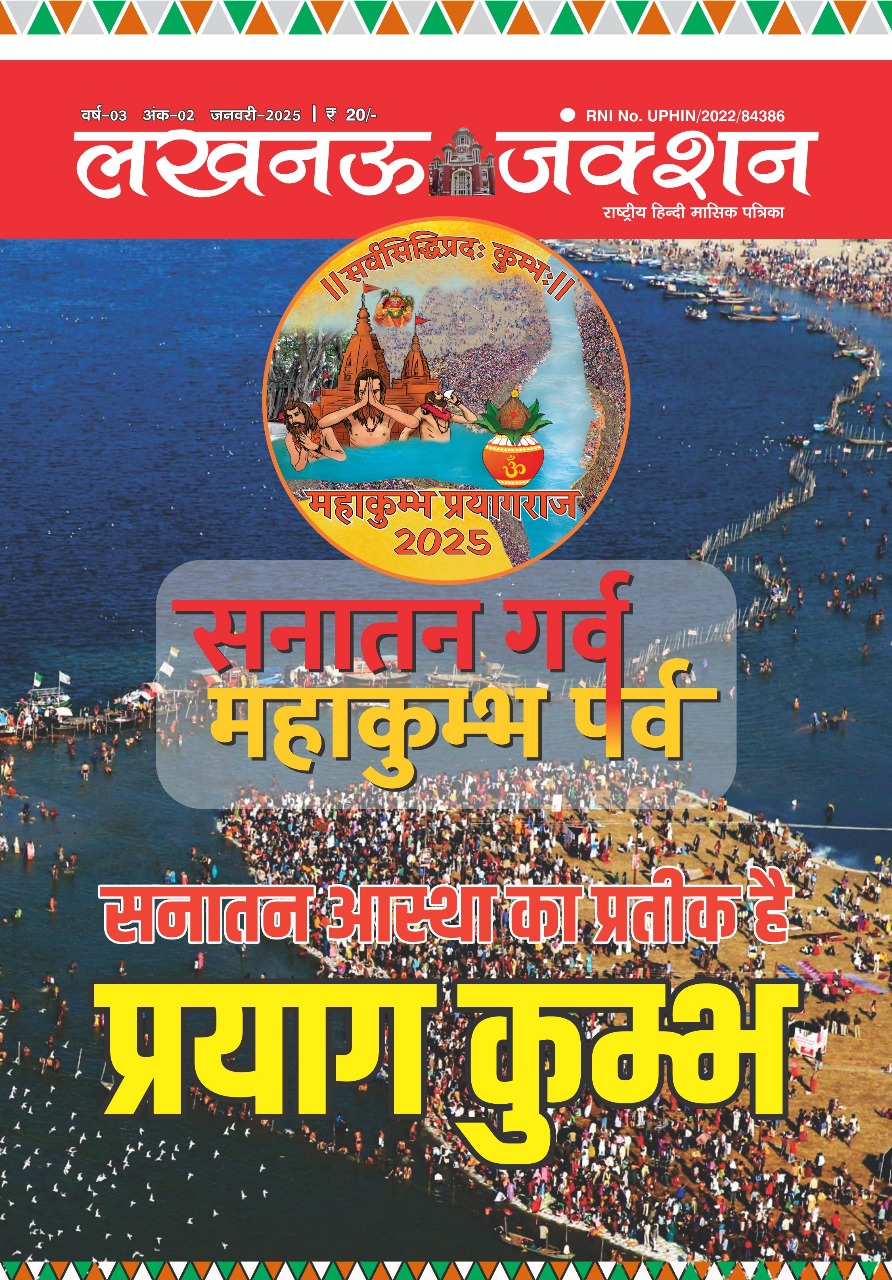स्वतंत्रता के बाद से देश में पर्यावरण विज्ञान की यात्रा
विजय गर्ग
स्वतंत्रता के बाद से भारत में पर्यावरण विज्ञान की यात्रा तेजी से विकास, प्राचीन पारिस्थितिक ज्ञान और पर्यावरण क्षरण की बढ़ती चेतना के जटिल परस्पर क्रिया से जूझ रहे राष्ट्र की एक आकर्षक कहानी है। इस यात्रा को मोटे तौर पर कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक पर्यावरणीय मुद्दों के लिए एक अलग दृष्टिकोण की विशेषता है। 1.। प्रारंभिक वर्ष (1947 – 1970): पर्यावरण पर विकास तत्काल स्वतंत्रता के बाद के युग में, सरकार का प्राथमिक ध्यान आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर था। प्रचलित दर्शन यह था कि अक्सर पर्यावरण की कीमत पर विकास राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक था। पर्यावरणीय चिंताएं नीति प्रवचन का एक प्रमुख हिस्सा नहीं थीं। कानूनी ढांचा काफी हद तक ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से एक कैरी-ओवर था, जिसमें 1927 के भारतीय वन अधिनियम जैसे कार्य थे। 2.। टर्निंग प्वाइंट: 1970 के दशक और पर्यावरण जागरूकता का उदय 1970 के दशक में भारत के पर्यावरण प्रक्षेपवक्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। इस दशक में कई प्रमुख घटनाओं और घटनाक्रमों का संगम देखा गया:
वैश्विक प्रभाव: स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर 1972 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक वाटरशेड क्षण था। इसने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंडा में पर्यावरणीय मुद्दों को सबसे आगे बढ़ाया। भारत एक भागीदार था और सम्मेलन ने सरकार को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और योजना परिषद की स्थापना के लिए प्रेरित किया।
प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन: 1970 के दशक में शक्तिशाली जमीनी आंदोलनों का उद्भव हुआ जिसने पर्यावरण के मुद्दों को जनता के ध्यान में लाया।
चिपको आंदोलन (1973): उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में उत्पन्न, इस आंदोलन ने ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं, पेड़ों को गले लगाते हुए देखा ताकि उन्हें वाणिज्यिक यात्रियों द्वारा गिर जाने से रोका जा सके। यह समुदाय के नेतृत्व वाले वन संरक्षण का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया।
द साइलेंट वैली मूवमेंट (1970 के दशक के अंत में): इस आंदोलन ने केरल की साइलेंट वैली में एक पनबिजली परियोजना का सफलतापूर्वक विरोध किया, जिसमें नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
विधायी परिवर्तन: इस नई जागरूकता ने विधायी गतिविधि की झड़ी लगा दी। 1972 का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम कानून का एक ऐतिहासिक टुकड़ा था जो जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया था। इसके बाद 1974 का जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, जो प्रदूषण को दूर करने वाला पहला व्यापक कानून था। 3। पर्यावरण शासन का संस्थागत रूप: 1980 का दशक 1980 के दशक में पर्यावरण ढांचे को और अधिक संस्थागत बनाने और मजबूत करने की अवधि थी।
भोपाल गैस त्रासदी (1984): इस औद्योगिक आपदा ने सख्त पर्यावरणीय नियमों और एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र की तत्काल आवश्यकता के गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। इसने सरकार को और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।
पर्यावरण और वन मंत्रालय (1985): राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और योजना परिषद को एक पूर्ण मंत्रालय, (अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) में अपग्रेड किया गया था। इसने पर्यावरण संरक्षण को विनियमित करने और सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित प्रशासनिक निकाय की स्थापना की।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: यह अधिनियम भोपाल त्रासदी का सीधा जवाब था। यह एक व्यापक कानून था जिसने केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोकने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया।
संवैधानिक संशोधन: पर्यावरण संबंधी चिंताओं को 42 वें संशोधन (1976) के साथ संवैधानिक मंजूरी दी गई, जिसमें अनुच्छेद 48 ए (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) और अनुच्छेद 51-ए (जी) (मौलिक कर्तव्य) को जोड़ा गया, जिससे यह राज्य और पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बन गया। 4। सतत विकास और सार्वजनिक भागीदारी का युग: 1990 और परे 1990 के दशक और नई सहस्राब्दी में, सतत विकास की अवधारणा के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया गया।
न्यायिक सक्रियता: न्यायपालिका ने पर्यावरण शासन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। एक महत्वपूर्ण क्षण 1991 में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था जिसने पर्यावरण अध्ययन को शिक्षा के सभी स्तरों पर एक अनिवार्य विषय बना दिया। यह निर्णय पर्यावरण वकील एम.सी. द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) का परिणाम था। मेहता।
नया विधान: 2000 के दशक में कई महत्वपूर्ण कानूनों को पारित किया गया, जिनमें शामिल हैं:
** जैविक विविधता अधिनियम, 2002: जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इसके घटकों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना, और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करना।
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006: वन-निवास समुदायों के अधिकारों और वन संरक्षण में उनकी भूमिका को स्वीकार किया।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) (2010): एनजीटी को पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक विशेष न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरणीय मुद्दों के लिए त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5.। वर्तमान-दिन चुनौतियां और भविष्य की दिशा आज, देश में पर्यावरण विज्ञान और नीति विकसित होती रहती है। भारत सक्रिय रूप से वैश्विक जलवायु परिवर्तन पहल में लगा हुआ है और महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें शामिल हैं:
वायु और जल प्रदूषण: शहरी और औद्योगिक प्रदूषण प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं हैं।
जैव विविधता हानि और आवास क्षरण: तेजी से शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से भारत की समृद्ध जैव विविधता को खतरा है।
अपशिष्ट प्रबंधन: ठोस, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन एक बढ़ती चुनौती है।
जलवायु परिवर्तन प्रभाव: देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जैसे कि चरम मौसम की घटनाएं, समुद्र-स्तर में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा मुद्दे। स्वतंत्रता के बाद से भारत में पर्यावरण विज्ञान की यात्रा एक गैर-मुद्दे से राष्ट्रीय नीति के केंद्रीय स्तंभ में बदल गई है, जो सार्वजनिक आंदोलनों, विधायी कार्रवाई और न्यायिक हस्तक्षेप के संयोजन से प्रेरित है। आगे के मार्ग के लिए अभिनव समाधान, सार्वजनिक जागरूकता और राष्ट्रीय विकास के सभी पहलुओं में पर्यावरणीय चिंताओं के एकीकरण पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद् स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब -152107 मोबाइल 9465682110
[1)