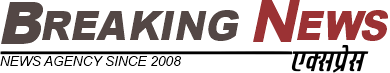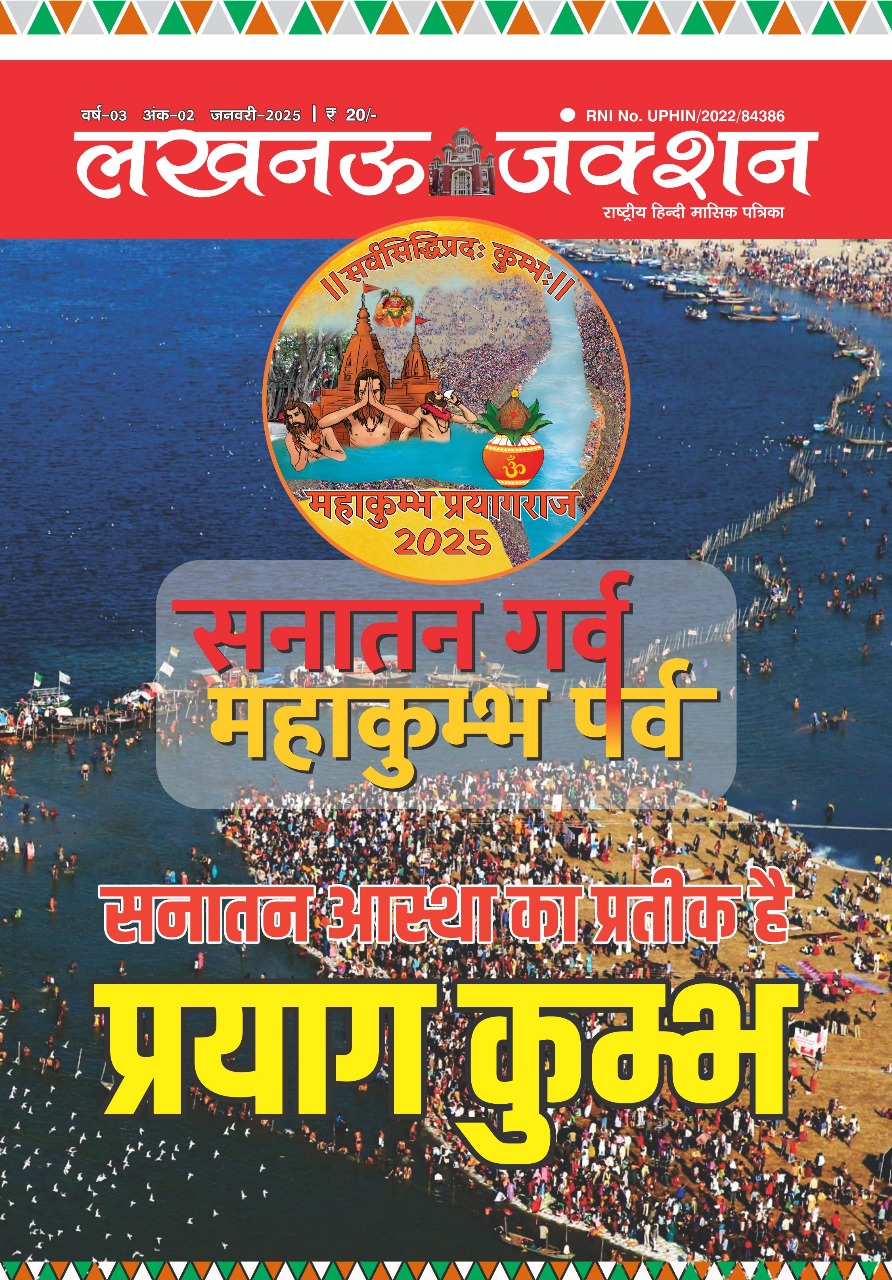भाषाई विविधता का सौंदर्य
विजय गर्ग
भारत को विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। यहां सांस्कृतिक वैविध्य का अनूठापन है। देश में संस्कृति के कई पहलू जैसे खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन और बोली-भाषा में भिन्नता के स्वरूप का सौंदर्य देखने को मिलता है। भाषा किसी संस्कृति की संवाहिका होती है और यह संस्कृति के सौंदर्य को निखारती है। किसी एक भाषा को जानना वहां की पूरी संस्कृति से परिचय करना होता है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में भाषाई विवाद को तूल दिया गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे। अभी भी बाजार में, ट्रेन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के विवाद देखने को लगातार मिल रहे हैं। इससे पहले बंगलुरु जैसे शहर में भी स्थानीय भाषा को लेकर विवाद हो चुके हैं, जहां बहुत बड़ी आबादी वहां की मूल निवासी नहीं है। राजनीति से प्रेरित होकर तमिलनाडु सदैव हिंदी का विरोध करता रहा है। ऐसे में भाषाएं अगर एक- दूसरे की विरोधी होने लगेंगी तो वैविध्य में जो सौंदर्य रहा है, जिस वजह से भारत को विविधताओं का का अनुपम देश कहा जाता है, उस छवि को नुकसान होगा और सांस्कृतिक रूप से हम कमजोर होंगे। इसके पीछे कई कारण हैं, जिन पर चर्चा करना आवश्यक गया है।
बहुधा ऐसे विवाद राजनीति से प्रेरित होते हैं। महाराष्ट्र में हाल में जो हुआ, उसे राजनीति के लिए भाषा के कंधे का इस्तेमाल कर और उसे अस्मिता से जोड़कर सामान्य लोगों को दिग्भ्रमित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। लोगों को धमकाने और मारपीट करने वाले विशेष राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जाहिर है कि वे सत्ता के केंद्र में नहीं करते हुए दिखना उनकी जरूरत है। सरकार जब तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाने के लिए कह रही है तो किसी भी कारण उसका विरोध करना मानो उनका नैतिक दायित्व बन जाता है। महाराष्ट्र में पहली से पांचवीं कक्षा तक हिंदी भाषा को मराठी और अंग्रेजी बाद तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और अब यह पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। सरकार ने त्रिभाषा सूत्र को अपनाते हुए अपनी अधिसूचना में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप अनिवार्य कर दिया था। हालांकि, विवाद के बाद अनिवार्य शब्द को हटा लिया गया।
मराठी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के में पढ़ाया जाएगा। यहां एक अच्छी
लिए बात यह रही कि अगर विद्यार्थी हिंदी अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी, बशर्ते ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बीस से कम न हो। हिंदी की अनिवार्यता को लेकर अन्य अस्मिताएं जागृत हो जाती हैं, लेकिन अंग्रेजी के वर्चस्व को लेकर इस तरह के विवाद प्रायः नहीं देखने को मिलते इसके पीछे एक कारण तो देश की राजनीति का बड़ा हिस्सा हिंदी क्षेत्र का है, इसलिए राजनीतिक रूप से खतरा हिंदी क्षेत्र से लगता । जबकि अंग्रेजी भारतीय भाषा न होने के कारण अस्मिता संबंधी कोई प्रश्न इससे जुड़ नहीं पाता और यही कारण है कि अंग्रेजी इस मामले में सुरक्षित रहती है।
क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर यह मुद्दा भावनाओं से भी जुड़ जाता है, इसलिए सामान्य भोले-भाले लोगों को जब यह बात कह कर प्रभावित किया जाता है कि आप अपने ही क्षेत्र में धीरे-धीरे भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो उनका डर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। डर का अपना
मनोविज्ञान होता है, जो बहुत तेजी से कार्य करता है। साथ ही उनके अंदर यह भाव भी भरा जाता है कि दूसरी भाषा के लोग आपके क्षेत्र के
संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी नौकरियों पर अधिकार जमा रहे हैं। यह सब तब हो रहा है, जब संविधान पूरे देश में निर्बाध रूप से घूमने, रहने और रोजगार पाने आदि का अधिकार देता है।
इस विवाद का दूसरा पहलू भी महत्त्वपूर्ण है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब त्रिभाषा सूत्र को व्यवहार में लाया जा रहा था तो उत्तर भारत में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त लगभग सभी जगहों पर विद्यार्थी तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ रहे थे। यह विद्यालयों में आम व्यवहार रूप में अपनाया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत पढ़ी जाती रही। इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि जिन दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा हिंदी का विरोध दर्ज कराया जाता है, उनकी भाषा को उत्तर भारतीयों द्वारा कभी सीखने का गंभीर प्रयास नहीं किया गया। यह एक प्रमुख कारण रहा, जिस वजह से हिंदी क्षेत्र ने अपना भरोसा कायम नहीं किया और जब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बहस चली, तो सदैव वहां से तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लोग एक-दूसरे की संस्कृति से कम ही परिचित रहे।
इतिहास में अगर देखा जाए तो आजादी से पूर्व हिंदी से इतर क्षेत्रों के बड़े नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन दिया। सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का है। इसके अलावा बंगाल में केशव चंद्र सेन, दक्षिण में मोदुरी सत्यनारायण, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और वीर र ने भी हिंदी की ही वकालत की। यही एक भाषा थी, जो सबको जोड़ सकती थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद इसे भुला दिया गया और हिंदी की राष्ट्रभाषा की मांग की स्थिति कमजोर होती चली गई। अगर वर्ष 2011 1 को देखें तो 43 फीसद लोगों की प्राथमिक भाषा हिंदी सावरकर
की जनगणना की है, लेकिन राष्ट्रभाषा वाला पहलू अब राजनीति से प्रेरित हो गया है। इस बार की जनगणना जो होने वाली है, उसमें इसकी संभावना | थोड़ी सकती है, क्योंकि हिंदी क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है।
यों भाषा का कार्य जोड़ने का है, लेकिन इसे सही दिशा नहीं दी जाए तो यही भाषा तोड़ने का भी कार्य कर सकती है। जैसा अभी हाल के विवादों में देखने को भी मिल रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा के साथ-साथ दूसरे की भाषा का सम्मान करें। सहअस्तित्व का भाव हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपनी भाषा से हम अपनी संस्कृति का परिचय प्राप्त करते हैं. हैं, तो दूसरी भाषा से दूसरी संस्कृति का यह क्रम हमें देश की अन्य समृद्ध संस्कृतियों से परिचय का अवसर देता है। इससे खुद को और बेहतर बनाने का मार्ग भी खुलता है।
भाषा के नाम पर अगर इस तरह के विवाद आगे बढ़ते जाएंगे तो वैविध्य का सौंदर्य धीरे-धीरे नष्ट होता जाएगा जिस विविधता की वजह से भारत दुनिया भर में जाना जाता है, वह साख खत्म हो जाएगी। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तो वैसे भी विविधता को नष्ट कर सब कुछ एक तरह का कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसा न हो कि विविधता में एकता महज एक खोखला नारा बनकर रह जाए, इसलिए हम सभी को उदारमन से एक-दूसरे की भाषा का सम्मान करना चाहिए। साथ ही यह कोशिश करनी चाहिए कि अपनी भाषा के अतिरिक्त एक और अन्य भारतीय भाषा अवश्य सीखी जाए।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब
++-++++++++