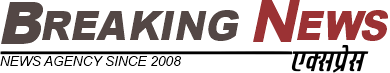ष्ण कुमार यादव-पोस्टमास्टर जनरल,
Breaking news express
विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर पर विशेष-कोई लौटा दे वो चिट्ठियाँ
चिट्ठियाँ लिखना और पढ़ना किसे नहीं भाता। शब्दों के विस्तार के साथ बहुत सी अनकही भावनाएं मानो इन चिट्ठियों में सिमटती जाती थीं। आपको याद है, आपने अंतिम बार कब पत्र लिखा था ? वह लाल रंग का लेटर बाक्स याद है, जिसे हम बचपन में हनुमान जी का प्रतिरूप समझते थे, कि यह हमारे डाले गए पत्रों को रात में उड़कर गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते हैं। न जाने कितनी बार स्कूल के दिनों में परिजनों को रात में जागकर चिट्ठियाँ लिखी होंगीं। पर आज इंटरनेट, ई-मेल, मोबाईल, वाट्सएप और सोशल मीडिया ने मानो पत्रों की दुनिया ही बदल दी हो। प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार लॉर्ड बायरन पत्र को एकांत का साथी मानते थे। उनका मानना था कि अगर तुम एकांत में सबसे अच्छे मित्र की तलाश में हो, तो अपने किसी को पत्र लिखो।यह जीवन की धूप-छांव में सबसे ईमानदारी भरा पल होगा, जो तुम्हें अपने सबसे करीब ले पाएगा। बायरन का कहना था कि पत्र लेखन एक प्रकार का चिंतन है, जो मस्तिष्क को स्थिरता देता है। पत्र लिखना जितना मायने रखता है, उतना ही उसे पढ़ना भी।
सभ्यता के आरम्भ से ही मानव किसी न किसी रूप में पत्र लिखता रहा है। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पत्र 2009 ईसा पूर्व का बेबीलोन के खण्डहरों से मिला था, जोकि वास्तव में एक प्रेम पत्र था और मिट्टी की पटरी पर लिखा गया था। कहा जाता है कि बेबीलोन की किसी युवती का प्रेमी अपनी भावनाओं को समेटकर उससे जब अपने दिल की बात कहने बेबीलोन तक पहुँचा तो वह युवती तब तक वहाँ से जा चुकी थी। वह प्रेमी युवक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और उसने वहीं मिट्टी के फर्श पर खोदते हुए लिखा-‘‘मैं तुमसे मिलने आया था, तुम नहीं मिली।‘‘ यह छोटा सा संदेश विरह की जिस भावना से लिखा गया था, उसमें कितनी तड़प शामिल थी। इसका अंदाजा सिर्फ वह युवती ही लगा सकती थी जिसके लिये इसे लिख गया।भावनाओं से ओत-प्रोत यह पत्र 2009 ईसा पूर्व का है और इसी के साथ पत्रों की दुनिया ने अपना एक ऐतिहासिक सफर पूरा कर लिया है।
जब संचार के अन्य साधन न थे, तो पत्र ही संवाद का एकमात्र माध्यम था। दुनिया के किसी खामोश कोने में बैठकर दूसरे कोने में बैठे किसी अनाम साथी से संवाद, ऊष्मा से ज्यादा उत्तेजना का सबब हो जाता है। यह एकालाप नहीं बल्कि अकेलेपन से जोड़ने और अपनी संवेदनाओं को मजबूत करने का जरिया है। पत्रों का काम मात्र सूचना देना ही नहीं बल्कि इनमें एक अजीब रहस्य या गोपनीयता, संग्रहणीयता, लेखन कला एवं अतीत को जानने का भाव भी छुपा होता है।
पत्रों की सबसे बडी विशेषता इनका आत्मीय पक्ष है। यदि पत्र किसी खास का हुआ तो उसे छुप-छुप कर पढ़ने में एवम् संजोकर रखने तथा मौका पाते ही पुराने पत्रों के माध्यम से अतीत में लौटकर विचरण करने का आनंद ही कुछ और है।
पत्रों की दुनिया बेहद निराली है। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक यदि पत्र अबाध रूप से आ-जा रहे हैं तो इसके पीछे ‘यूनिवर्सल पोस्टल‘ यूनियन का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को स्विटजरलैंड में हुई थी। यह 9 अक्टूबर पूरी दुनिया में ‘विश्व डाक दिवस‘ के रूप में मनाया जाता है। तब से लेकर आज तक डाक-सेवाओं में वैश्विक स्तर पर तमाम क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं और भारत भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं हैं। डाक सेवाओं का इतिहास बहुत पुराना है, पर भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्तूबर 1854 को लार्ड डलहौजी के काल में हुई। डाकघरों में बुनियादी डाक सेवाओं के अतिरिक्त बैंकिंग, वित्तीय व बीमा सेवाएं भी उपलब्ध हैं। एक तरफ जहाँ डाक-विभाग सार्वभौमिक सेवा दायित्व के तहत सब्सिडी आधारित विभिन्न डाक सेवाएं दे रहा है, वहीं पहाड़ी, जनजातीय व दूरस्थ द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में भी उसी दर पर डाक सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।
आजादी के आन्दोलन में भी चिट्ठियों का बड़ा योगदान रहा है। इस दौर में तमाम क्रान्तिकारी नायकों ने भी बड़ी संख्या में हरकारों की भर्ती कर रखी थी, जो उनके लिए गुप्त खबरें भी लाते थे। कानपुर में नाना साहब के दरबार में एक हरकारे गिरधारी ने ही मेरठ विद्रोह की खबर सर्वप्रथम पहुँचाई थी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। यह अनायास ही नहीं था कि 1857 के बाद से डाकघर और डाकिये बराबर क्रान्तिकारियों के निशाने पर रहे। 1857 की क्रान्ति के दौरान जब क्रान्तिकारियों ने कानपुर में अंग्रेजों की संचार व्यवस्था ध्वस्त कर दी तो सेनापति कोलिन थेंप विल ने पत्र द्वारा गर्वनर जनरल लार्ड केनिंग को यहाँ के
बारे में सूचित करते हुए सलाह दी कि जब तक अंग्रेजी सेनायें अवध को काबू में नहीं करेंगी, तब तक क्रान्ति की चिंगारी यूँ ही फैलती रहेगी। कालान्तर में भी डाकिये लोगों के निशाने पर रहे,क्योंकि अंग्रेजों के पास संचार माध्यम का यह सबसे सशक्त साधन था।
पत्रों को सही जगह पहुँचाने का डाकियों का गुण किसी से भी नहीं छुपा है। गाँधी जी के पास तो रोज सैकड़ों पत्र आते थे और वे व्यक्तिगत रूप से इन सभी का जवाब देते थे।महात्मा गाँधी तो पत्र लिखने में इतने सिद्धहस्त थे कि दाहिने हाथ के साथ-साथ वे बाएं हाथ से भी पत्र लिखते थे। डाक विभाग भी इतना मुस्तैद था कि मात्र ’’गाँधी जी’’ लिखे पते के आधार पर उन्हें कहीं भी चिट्ठियाँ पहुँचा देता था। यह अनायास ही नहीं है आज भी डाक-टिकटों पर भारत में सबसे ज्यादा गाँधी जी के ही दर्शन होते हैं। पं. जवाहर लाल नेहरू अपनी पुत्री इन्दिरा गाँधी को जेल से भी पत्र लिखते रहे। ये पत्र सिर्फ पिता-पुत्री के रिश्तों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें तात्कालिक राजनैतिक एवं सामाजिक परिवेश का भी सुन्दर चित्रण है। इन्दिरा गाँधी के व्यक्तित्व को गढ़ने में इन पत्रों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज ये किताब के रूप में प्रकाशित होकर ऐतिहासिक दस्तावेज बन चुके हैं। इन्दिरा गाँधी ने इस परम्परा को जीवित रखा एवं दून में अध्ययनरत अपने बेटे राजीव गाँधी को घर की छोटी-छोटी चीजों और तात्कालिक राजनैतिक-सामाजिक परिस्थितियों के बारे में लिखती रहीं। एक पत्र में तो वे राजीव गाँधी को रीवा के महाराज से मिले सौगातों के बारे में भी बताती हैं। तमाम राजनेताओं-साहित्यकारों के पत्र समय-समय पर पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होते रहते हैं। इनसे न सिर्फ उस व्यक्ति विशेष के संबंध में जाने-अनजाने पहलुओं का पता चलता है बल्कि तात्कालिक राजनैतिक-सामाजिक-साहित्यिक-सांस्कृतिक परिवेश के संबंध में भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसी ऐतिहासिकता के कारण आज भी पत्रों की नीलामी लाखों रूपयों में होती हैं। तभी तो दिलीप कुमार ने ‘ब्लैक‘ फिल्म
देखने के बाद अमिताभ बच्चन को जो बधाई पत्र लिखा था, उस पत्र को अमिताभ ने अपने ड्रांइग रूम में सजा दिया है।पत्रों को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं। हम सभी ने वो वाली कहानी सुनी है,जिसमें एक किसान पैसों के लिए भगवान को पत्र लिखता है और उसका विश्वास कायम रखने के लिए पोस्टमास्टर अपने स्टाफ से पैसे एकत्र कर उसे मनीऑर्डर करता है। आर. के. नारायण की एक कहानी है – पोस्टमैन। उसमें एक डाकिया किसी की मृत्यु के बारे में आई एक चिट्ठी लंबे समय तक अपने पास रोके रखता है क्योंकि गाँव में एक लड़की की शादी की तैयारियां चल रही हैं। चिट्ठियों से हमारे समाज के भावनात्मक संबंध ने उसे हमारे साहित्य और सिनेमा में बखूबी स्थान दिया है।
कहते हैं कि पत्रों का संवेदनाओं से गहरा रिश्ता है और यही कारण है कि पत्रों से जुड़े डाक विभाग ने तमाम प्रसिद्ध विभूतियों को पल्लवित-पुष्पित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन पोस्टमैन तो भारत में पदस्थ वायसराय लार्ड रीडिंग डाक वाहक रहे। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक व नोबेल पुरस्कार विजेता सी.वी. रमन भारतीय डाक विभाग में अधिकारी रहे वहीं प्रसिद्ध साहित्यकार व ‘नील दर्पण‘ पुस्तक के लेखक दीनबन्धु मित्र पोस्टमास्टर थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लोकप्रिय तमिल उपन्यासकार पी.वी. अखिलंदम, राजनगर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अमियभूषण मजूमदार, फिल्म निर्माता व लेखक पद्मश्री राजेन्द्र सिंह बेदी, मशहूर फिल्म अभिनेता देवानन्द डाक कर्मचारी रहे हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द जी के पिता अजायबलाल डाक विभाग में ही क्लर्क रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी ने आरम्भ में डाक-तार विभाग में काम किया था तो प्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉ. राष्ट्रबन्धु भी पोस्टमैन रहे। सुविख्यात उर्दू समीक्षक पद्मश्री शम्सुररहमान फारूकी, शायर कृष्ण बिहारी नूर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध किसान नेता शरद जोशी सहित तमाम विभूतियाँ डाक विभाग की गोद में अपनी सृजनात्मक-रचनात्मक काया का विस्तार पाने में सफल रहीं।
हाल ही में एक रिपोर्ट पर जाकर निगाह अटकी कि, जज्बातों को अल्फाज देती,कागज के कुछ पन्नों में सिमटी चिट्ठी लिखने की कला मानो खत्म सी होती जा रही है। ब्रिटेन में चैरिटी वर्ल्ड विजन द्वारा हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले करीब 50 फीसदी बच्चे ठीक से नहीं जानते कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती है। सात से लेकर 14 साल के बच्चों से पूछा गया कि क्या उन्होंने पिछले एक साल में चिट्ठियाँ लिखने की कोशिश की है तो चार में से एक बच्चे का जवाब था, नहीं। जबकि पिछले एक हफ्ते में इनमें से 50 फीसदी से ज्यादा बच्चों ने ईमेल किया है या सोशल नेटवर्किंग साइट पर संदेश भेजे हैं। अध्ययन से पता चलता है कि बहुत से बच्चे न तो चिट्ठियाँ लिखते हैं, न ही उन्हें किसी की चिट्ठी मिलती है।
आँकड़ों के मुताबिक पाँच में एक बच्चे को कभी किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी। करीब 45 फीसदी बच्चों ने कहा कि या तो उन्हें चिट्ठी लिखनी बिल्कुल नहीं आती या वे पक्के तौर पर नहीं कह सकते। ये सर्वेक्षण ब्रिटेन के 1188 बच्चों में किया गया। वाकई यह स्थिति सोचनीय है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े मामले की विशेषज्ञ सू पामर कहती हैं, ’’जब आप खुद कलम से कुछ लिखते हैं तो इसके जरिए लिखने वाला ये दर्शाता है कि वे उस रिश्ते को अपना वक़्त दे रहा है। तभी तो हम पुरानी चिट्ठियों को संभाल कर रखते हैं।’’
जब संचार के अन्य साधन न थे तो डाकिया लोगों के लिए देवदूत बनकर आता था। लोगों की निगाहें डाकिया बाबू का इंतज़ार करती थीं। डाकिया प्राकृतिक आपदाओं, जंगली जानवरों, भूभागी कठिनाइयों तथा डाकुओं आदि की बाधाओं को पार करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता था। रवींद्र नाथ टैगोर के नाटक ‘‘डाकघर‘‘ में चौकीदार द्वारा छोटे लड़के को इस तथ्य को कितनी अच्छी तरह बताया गया है- ‘‘हा…हा….डाकिया, यकीनन बरसात हो या लू, अमीर हो या गरीब, सबको घर-घर जाकर चिट्ठी बांटना उसका काम है यह बहुत बड़ी बात है।‘‘ वाकई चाहे बरसात हो या ठण्ड, डाकिया एक ही थैले में सुख और दुःख दोनों को बांटने वाला दूत समझा जाता था? तभी तो भूतपूर्व संचार मंत्री श्री स्टीफेन ने भोपाल में डाक-तार के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि-‘‘अगर स्वर्ग में एक जगह खाली हो और भगवान को सभी विभागों के कर्मचारियों में से किसी एक का चयन उस जगह के लिये करना हो तो वे ‘डाकिये‘ का ही चयन करेंगे क्योंकि उसने जीवन भर दूसरों के सन्देश घर-घर तक पहुँचाकर जो पुण्य कमाया है वह कोई दूसरा कर्मचारी नहीं कमा सकता।‘‘ उर्दू के जाने माने शायर निदा फाजली ने क्या खूब लिखा है-
सीधा-सादा डाकिया जादू करे महान ।एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान ।।प्रेम की बात की जाये और डाकिया का जिक्र न हो तो अधूरा सा लगता है।
कालिदास ने तो अपने प्रेम के लिए मेघों को ही दूत बना लिया, पर वास्तविक जीवन में भी डाकियों ने प्रेम-दूत का काम बखूबी निभाया है। याद कीजिये वह हिंदी फिल्म का गीत जिसमें नायिका दूर शहर चले गए अपने प्रेमी को खत लिखने के लिए डाकिया से मिन्नतें करती है-खत लिख दे सांवरियां के नाम बाबू ।कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू ।।वो जान जाएंगें, वो मान जाएंगें –कैसे होती है सुबह से शाम बाबू ।।इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के इस दौर में युवा पीढ़ी भले ही डाकिया को अपने लिए अनजाना समझती हो, पर डाकिया आज भी प्राय: हर दरवाजे पर दस्तक लगाता है।संचार क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में सन्देश भेजने के तमाम साधन इन डाकियों के सामने ही दम तोड़ते चले गए, पर डाकिया का अस्तित्व अभी भी कायम है। पुराने जमाने के टेलीग्राफ से लेकर नए दौर के पेजर तक की सेवाएँ ख़त्म हो गईं, टेलीफोन की जगह मोबाईल ने ले ली और एस. एम. एस. का वजूद वाट्सएप ख़त्म कर गया, पर चिट्ठी-पत्री का दौर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। डाकिया के थैले में व्यक्तिगत पत्रों की बजाय अब सरकारी डाक, कॉरपोरेट डाक,पत्र-पत्रिकाओं, पार्सल की संख्या भले ही बढ़ गई हो, पर बदलते दौर के साथ डाकियों की भूमिका भी बदल रही है। । इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना के बाद आर्थिक और सामाजिक समावेशन के तहत ग्रामीण पोस्टमैन चलते-फिरते एटीएम के रूप में नई भूमिका निभा रहा है।
आई. टी. मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से डाकिया अपनी नई भूमिका को नई चुनौतियों के साथ स्वीकारने को तत्पर है और निश्चितत: डिजिटल इण्डिया, वित्तीय समावेशन से लेकर न्यू इंडिया तक की संकल्पना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में डाकियों की अहम भूमिका है।चिट्ठियों से चिट्ठों और सोशल नेटवर्किंग साइट्स तक के इस सफर में बहुत कुछ बदला है, आगे भी बदलेगा। हाई-टेक होते इस दौर में कलम का स्थान की-बोर्ड ने ले लिया है।शब्दों के भावार्थ बदलने लगे हैं, उनमें शुद्धता नहीं बल्कि चलताऊपन आ गया है। पर जब यही बात रिश्तों-संवेदनाओं पर लागू होती है तो असहजता महसूस होती है। चिट्ठियाँ लिखना कम हुआ तो लिफाफा देख मजमून भांपने वाली पूरी जमात का अस्तित्व खतरे में है। मोबाइल फोन और कम्प्यूटर से कुछ भांपा नहीं जा सकता। पर इन सबके बीच यह बेहद जरूरी है कि संवेदनाएं अपना रूप न परिवर्तित करें। टेक्नालाजी ने दिलों की दूरियाँ इतनी बढ़ा दी हैं कि बिल्कुल पास में रहने वाले अपने इश्ट मित्रों और रिश्तेदारों की भी लोग खोज-खबर नहीं रखते। ऐसे में युवा पीढ़ी के अंदर संवेदनाओं को बचा पाना कठिन हो गया है। तभी तो पत्रों की महत्ता को देखते हुए एन.सी.ई.आर.टी. को पहल कर कक्षा आठ के पाठ्यक्रम में ‘‘चिट्ठियों की अनोखी दुनिया‘‘ नामक अध्याय को शामिल करना पड़ा। चिट्ठियों/पत्रों को लेकर गाए गए न जाने कितने गीत आज भी होंठ गुनगुना उठते हैं। तभी तो अन्तरिक्ष-प्रवास के समय सुनीता विलियम्स अपने साथ भगवद्गीता और गणेशजी की प्रतिमा के साथ-साथ पिताजी के हिन्दी में लिखे पत्र ले जाना नहीं भूलती। हसरत मोहानी ने यूँ ही नहीं लिखा था-लिक्खा था अपने हाथों से जो तुमने एक बार।अब तक हमारे पास है वो यादगार खत ।।
कृष्ण कुमार यादव-पोस्टमास्टर जनरल,
उत्तरी गुजरात परिक्षेत्र, अहमदाबाद -380004
ई-मेलः kkyadav.t@gmail.com
_____________________________________________________________________